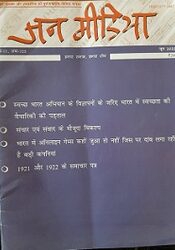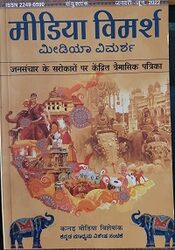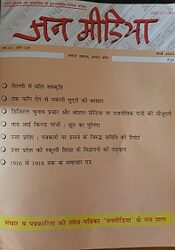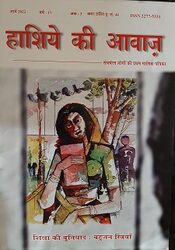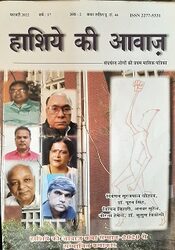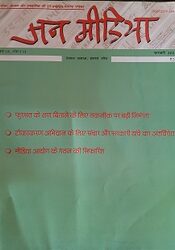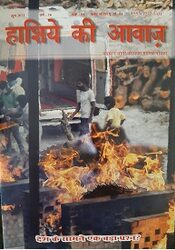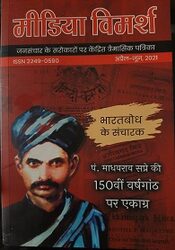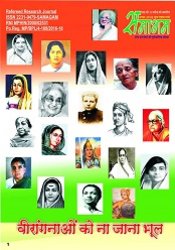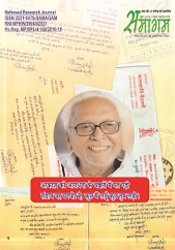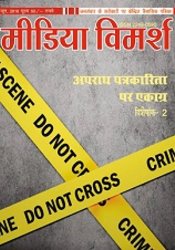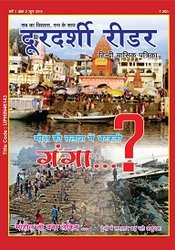विष्णु नागर। जिंदगी भर हिंदी पत्रकारिता की। हिंदी अखबारों का आज का मानसिक दिवालियापन, सरकार की जीहुजूरी, हिंदुत्व का प्रोपेगैंडा और हिंदी को विकलांग बनाने की साजिश सी इस भाषा के अखबारों तथा टीवी चैनलों पर दिखाई पड़ती है, वह व्यथित करती है। गोदी चैनल तो दिनरात नफरत की मशीनगन बने हुए हैं। कोई रोकटोक, कहीं से नहीं। विपक्ष भी बोलता नहीं। अखबार भी अधिकतर ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता, किसे खरीद जाए? न खबर जैसी कोई खबर उनमें। न अधिकांश में ढँग का कोई लेख। भाषा का सत्यानाश अलग से कर रहे हैं। हिंदी में हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा है। भाषा से बरताव कैसे किया जा सकता है, इसका अहसास तक नहीं।
विष्णु नागर। जिंदगी भर हिंदी पत्रकारिता की। हिंदी अखबारों का आज का मानसिक दिवालियापन, सरकार की जीहुजूरी, हिंदुत्व का प्रोपेगैंडा और हिंदी को विकलांग बनाने की साजिश सी इस भाषा के अखबारों तथा टीवी चैनलों पर दिखाई पड़ती है, वह व्यथित करती है। गोदी चैनल तो दिनरात नफरत की मशीनगन बने हुए हैं। कोई रोकटोक, कहीं से नहीं। विपक्ष भी बोलता नहीं। अखबार भी अधिकतर ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता, किसे खरीद जाए? न खबर जैसी कोई खबर उनमें। न अधिकांश में ढँग का कोई लेख। भाषा का सत्यानाश अलग से कर रहे हैं। हिंदी में हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा है। भाषा से बरताव कैसे किया जा सकता है, इसका अहसास तक नहीं।
अधिकतर संपादक, संपादक नहीं रहे। मालिक और मैनेजर के गुलाम हैं। कुछ तो साफ- साफ दलाली का धंधा करते हैं। हर अखबार लगभग एक जैसा खराब है। कोई दस प्रतिशत अच्छा है, दूसरे से। कोई बीस प्रतिशत और खराब है, दूसरे से। खराब ही लोकप्रिय है,बिकता वही है।
सरकारी दबाव के बावजूद अधिकतर अंग्रेजी अखबार फिर भी अखबार से लगते हैं।कुछ पढ़ने- समझने को उनमें मिलता है। हिंदी अखबार में सप्ताह में दो लेख भी ढँग के मिल जाएँ तो समझिए धन्य हुए। बाकी अखबारों पर भी काफी दबाव है कि किसी लेख में एक पंक्ति तक ऐसी न जाए, जिसके सरकार विरोधी होने का आभास तक हो। मेरे कुछ दोस्त अभी भी अखबारों में नियमित रूप से लिखते हैं मगर डर- डर के,बच-,बच के,फूँक फूँक के। एकाध बार थोड़ी हिम्मत कोई दिखा दे तो फौरन आईटी सेल के बंदे सक्रिय होकर अखबार पर ,लेखक पर दबाव बना देते हैं।या तो इसका लिखना बंद करवाओ या इससे कहो, सीधी राह पर चले। इधर उधर न देखे। आँखें बंद रखे,बौद्धिकता-विद्वत्ता के चक्कर में न पड़े। जो थोड़े बहादुर से हैं,वे भी अमूर्तन में बात करते हैं। लिखने की शर्त यही है।
पहले कम से कम छोटे -बड़े कुछ विकल्प हुआ करते थे। खराब अखबार को भी काफी हद तक खुला और बेहतरीन बना देने वाले संपादक हुआ करते थे। मालिक, मैनेजर और सरकार खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं खेलते थे।अब कुछ छिपालुका नहीं है।रामराज्य है। सब ओर जयश्री राम है।
ये भी अच्छा हुआ कि परसाई जी और शरद जी जैसे व्यंग्यकार समय से जन्म लेकर समय से चले गए वरना आज व्यंग्य लिखने की जिद पर अड़े रहते तो दाल- रोटी के भी लाले पड़ जाते!