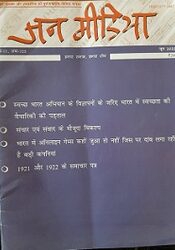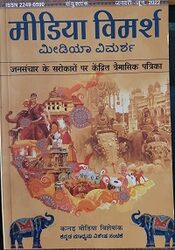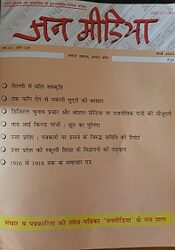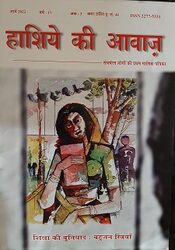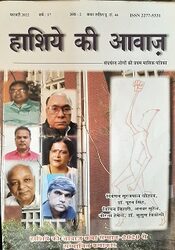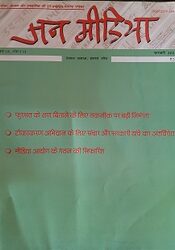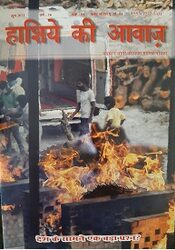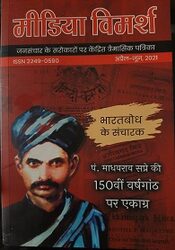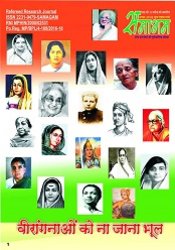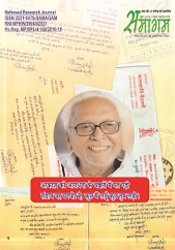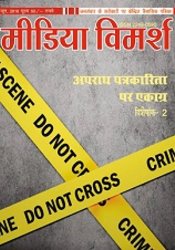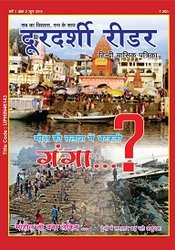मीडिया में न सिर्फ दलितों- पिछड़ो की उपस्थिति न के बराबर है बल्कि इनकी समस्याएं भी मीडिया में अनुपस्थित हैं प्रख्यात चिंतक और आलोचक वीरेन्द्र जी का यह व्याख्यान इस इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है
मीडिया में न सिर्फ दलितों- पिछड़ो की उपस्थिति न के बराबर है बल्कि इनकी समस्याएं भी मीडिया में अनुपस्थित हैं प्रख्यात चिंतक और आलोचक वीरेन्द्र जी का यह व्याख्यान इस इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है
कैसा है हमारा मीडिया ? इस मीडिया में मुकम्मल भारत की तस्वीर नही हैं, गांव नहीं है, हाशिये का समाज नहीं है। मीडिया में दलितों के साथ दलित समस्याएं भी अनुपस्थित हैं। आज समाज को समग्र नजरिये से देखने की जरूरत है। दलितों की उपस्थिति के साथ, दलित समाज के आलोचना की जरूरत के लिए भी मीडिया में दलितों की आवश्यकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली पर सामाजिक जनतंत्र ? एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है । वह है सामाजिक जनतांत्रिकीकरण का। इसके लिए भारत में सामाजिक जनतंत्र स्थापित करना ही होगा। इसके बिना जनतंत्र का क्या अर्थ ?
मीडिया में दलित का मुद्दा इन सारे से प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। यह महज आरक्षण का या प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है या जनतंत्र को लेकर मीडिया का यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। संजय कुमार की किताब में रॉबिन जाफरी का जिक्र आया है। वे वाशिंगटन पोस्ट के नई दिल्ली में संवाददाता रहे थे और अपनी एक स्टोरी के सिलसिले में वे चाहते थे कि किसी दलित पत्रकार से बात करें। इस सम्बन्ध में उन्होंने पीआईबी से सम्पर्क किया और दलित पत्रकारों का विवरण मांगा। लेकिन एक भी दलित पत्रकार पीआईबी की लिस्ट में उन्हें नहीं मिला। सैकड़ों मान्यता प्राप्त पत्रकार पीआईबी की लिस्ट में है लेकिन देश के एक भी दलित का नाम सूची में नहीं मिलना चौकानें वाली बात थी। उन्होंने इस पर वाशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखा और अपने दिल्ली के पत्रकार मित्र बी.एन.उनियाल से बात की। उनियाल ने" दि पॉयनियर " में एक खबरनुमा स्टोरी लिखकर इस समूचे प्रकरण का जिक्र किया। इसके बाद योगेन्द्र यादव ने अपनी सी एस डी एस की टीम के सर्वेक्षण द्वारा इस बात का खुलासा किया कि देश की राजधानी दिल्ली में जो प्रिंट और मीडिया हाउस है वहां निर्णय लेने वाले पदों पर 90 प्रतिशत द्विज समाज के लोग काबिज है। बाकी 10 प्रतिशत में दूसरे लोग है और किसी भी निर्णायक पद पर दलित या शूद्र नहीं है। इस तथ्य के खुलासा होने से इस पर लंबी बहस शुरू हो गयी, उस वक्त दैनिक हिन्दुस्तान की संपादक मृणाल पाण्डेय ने सर्वे पर 'जाति 'तलाशने का आरोप मढ़ते हुए एक लेख लिखा ’जाति न पूछो साधो की..'.....।
मीडिया में दलित उपस्थित नहीं है और जब मीडिया में गैरद्विजों की उपस्थिति या दलितों की उपस्थिति का सवाल उठाया गया तो मीडिया के वर्चस्वशाली लोगों द्वारा उसका एक प्रतिकार और प्रतिरोध किया गया। यह तर्क भी दिया गया कि मीडिया मालिकों का किसी तरह का निर्देश नहीं है कि हम दलितों या निम्न वर्गों से आये लोगों की नियुक्ति न करें। अगर योग्य नहीं मिलते है तो हम क्या करें ? लेकिन एक उदाहरण मौजूद है सिद्धार्थ वर्द्धराजन का जो, आज ‘हिन्दू’ के संपादक हैं। वे जब रिर्पोटिग करते थे तब चेन्नई की एक घटना का हवाला दिया। जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि दलितों की समस्याओं को लेकर अखबारों में कितनी शोचनीय स्थिति है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा कि एक मेडिकल कॉलेज के दलित छात्रों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए आंदोलन किया और हड़ताल पर चले गये। इसकी खबर एक भी समाचार पत्र में नहीं छपी। दलित छात्रों का प्रतिनिधि अखबारों में गया और उन्हें बताया भी, फिर भी खबर नहीं आयी। वे सिद्धार्थ वर्द्धराजन से मिले, अपनी बातें बतायी। वरदराजन ने शहर के संस्करण प्रभारी को खबर छापने को लेकर चर्चा की । प्रभारी ने रिपोर्टर भेजने की बात कही। लेकिन रिपोर्टर को नहीं भेजा गया। कई दिन बीत गये लेकिन खबर नहीं आयी। तब उन्होंने ने अपने सीनियर से रिपोर्टर भेजकर समाचार कवरेज के लिए कहा, इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। स्वयं सिद्धार्थ वर्द्धराजन मेडिकल कॉलेज गये और दलित छात्रों के साथ भेदभाव पर पूरी रिपोर्ट तैयार की और छपने के लिए अखबार को दे दिया। वह स्टोरी एक हफ्ते तक नहीं छपी। जब स्टोरी नहीं छपी तो उन्होंने संपादक से कहा। कई दिनों के बाद जब दलित छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया तो वह स्टोरी छपी। सिद्धार्थ वर्द्धराजन ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि स्थिति यह है कि अख़बारों में दलित की उपस्थिति तो है ही नहीं और दलितों की अनुपस्थिति के साथ-साथ दलित समस्याएं भी इस तरह से अनुपस्थित है।
तमिलनाडु के ही एक अंग्रेजी में जब एक दलित साक्षात्कार देने गया तो उससे सवाल समाज-देश-पत्रकारिता के बारे में न पूछकर यह पूछा गया कि आप किस इलाके से आते हैं ? जब उस दलित उम्मीदवार ने अपने निवास के इलाके का नाम बताया तो कहा गया वहां तो अमुक जाति के लोग हैं तो क्या तुम उस जाति के हो ! जब दलित उम्मीदवार ने कहा नहीं तो वे जान गये कि ये दलित है। सामने वाला किस जाति- समाज का है ? इस तरह से नियुक्ति। कहा जा सकता है कि यह एक प्रभुत्वशाली प्रवृति व मनोदशा है। यानी जो माईंडसेट है, माहौल है, वह दलित विरोधी है। जो अपने आप एक दर्द है।
1975 के आसपास अमेरिका की पत्रकारिता में ब्लैक की स्थिति बहुत कम थी। इसे लेकर कुछ लोग आगे आये। मीडिया में अश्वेतों की कम उपस्थिति पर चर्चा की गयी। संपादकों की बैठकें हुई। एक आयोग गठित किया गया और तीन साल में उनके अनुपात को बढ़ाना तय किया गया । इसके लिए उन्होंने एक प्रक्रिया अपनाई। कुछ लोगों को विधिवत प्रशिक्षित किये जाने का फैसला हुआ। और फिर एक जर्नलिस्ट टैलेंट सर्च हुआ, यानी मीडिया में ब्लैक के प्रतिनिधित्व के लिए कार्यक्रम बना और नतीजा यह हुआ कि आज कई अखबारों के प्रभारी ब्लैक हैं। लेकिन भारतीय समाज में यह आज भी दिवास्वप्न सरीखा है ।
भारतीय मीडिया में दलित है ही नहीं तो करेंगे क्या ? जब सिद्धार्थ वर्द्धराजन दलितों की समस्याओं के लिए स्टोरी करते है और छपती नहीं है तो एकाध दलित को नौकरी मिल भी जाय तो इस तरह का जो मीडिया का व्यवहार है उसका क्या करेंगे? सवाल है कि मीडिया में व्यवस्थागत परिवर्तन का। वैकल्पिक मीडिया की बात होती रहती है, होती रहनी चाहिए और चलती रहनी चाहिए। लेकिन जो मुख्यधारा का मीडिया है उसे हम जनतांत्रिक कैसे बनाये, यह एक बड़ा सवाल है। इस मुख्यधारा के मीडिया में दलित समाज के लोगों की कैसे सम्मानजनक व प्रभावकारी उपस्थति दर्ज की जाये, यह भी एक बड़ा सवाल है। ग्राउंड लेबल पर यह स्थिति बनी हुई है कि दलित और आदिवासी हाशिये के समाज के लोग हैं। हाशिये के समाज के लोग इन माध्यमों में आते हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आ भी जायेंगे तो करेंगे क्या ?
हाल ही में एक पुस्तक आयी है " अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया " जो भारत के ग्यारह राज्यों के सर्वे पर आधारित है। सर्वे में कहा गया है कि भारतीय समाज में किस-किस तरह से दलितों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। सर्वे बताता है कि आज भी भारत के 80 प्रतिशत गांव में किसी न किसी रूप में दलितों के साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है। पंचायत में नीचे बैठने को कहा जाता है। मीड डे मील को लेकर भेदभाव किया जाता है। चार में से एक गांव आज भी ऐसे है जिनमें नये कपड़े, छाता लेकर चलने और चश्मा लगाने, जूता पहनकर चलने पर दलितों को रोक है। शहर के दलितों के साथ शायद ऐसा नहीं हो! लेकिन आज भी यह हो रहा है। भारतीय समाज में खासकर दक्षिण भारत में कई ऐसे जगह है जहां पर ढाबों में दलितों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं। यह कहा जाता है कि आज ग्लोबलाइजेशन हुआ है मार्केट तंत्र आया है इससे कुछ सामाजिक समानता आई है। लेकिन जमीनी सच यह है कि आज भी गाँव के बाजार में जब दलित जाता है तो उसके साथ उसकी जातिगत पहचान बनी रहते है | दूसरे लोगों की तरह वह सामानों को अपने हाथ में उठा-उठा कर देखकर खरीद नहीं सकता, उसे दूर से ही दुकानदार को बताना होता है। सर्वे आधारित ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे आज के ग्रामीण भारत के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यह सच हमारे अखबारों में नहीं छपता। हिन्दी अखबारों में तो बिल्कुल नहीं। हिन्दी अखबारों में दलित तब उपस्थित होता है जब कोई बस्ती या गांव जला दिया जाता है। आज सांप्रदायिकता को तो बड़े खतरे के रूप में पहचाना गया लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है दलितों के साथ भेदभाव। यह भारतीय समाज का सच है। अंधेरे भारत का सच है, जो हमारे भारतीय मीडिया में अनुपस्थित है ।
दलित की उपस्थिति होगी तो कुछ संवेदनशीलता आयेगी। कल्पना कीजिए कि न्यूज रूम में 10 में से 9 द्विज समाज के लोग है। अगर 10 में से 9 दलित और शूद्र समाज के लोग हो, तो दलितों के मुद्दे सामने आयेंगे। यह मात्र दलित उपस्थिति का मुद्दा नहीं है बल्कि भारतीय समाज के जन्तान्त्रीकरन और समाजीकरण का भी मुद्दा है।
(पत्रकार संजय कुमार की पुस्तक ‘मीडिया में दलित ढ़ूंढ़ते रह जाओगे’ के लोकार्पण, यू पी प्रेस क्लब, लखनऊ के अवसर पर दिया गया व्याख्यान)
(वीरेंद्र जी के ब्लॉग देहरी http://gauravmahima.blogspot.in/2013/06/blog-post.html?spref=fb से साभार )