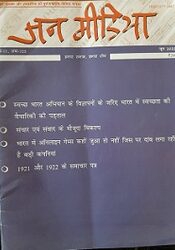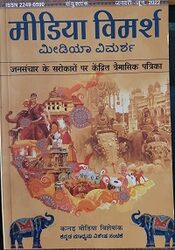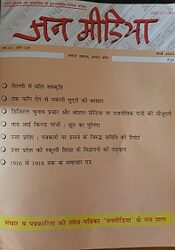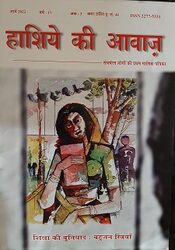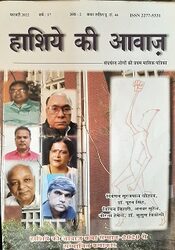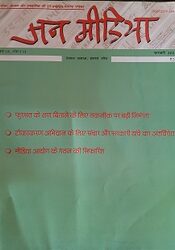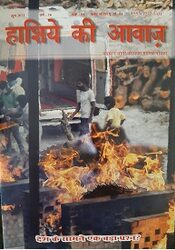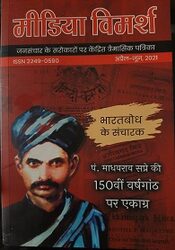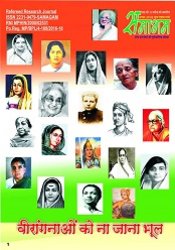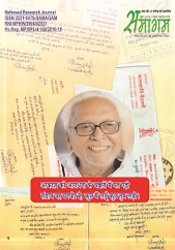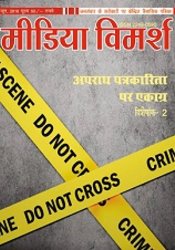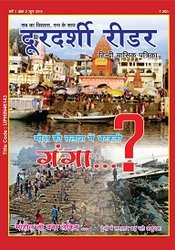मनोज कुमार/ सोशल मीडिया पर एक पीड़ादायक तस्वीर के साथ एक सूचना शेयर की जा रही है कि एक मजबूर पिता और एक मासूम बच्चा अपने भाई की लाश अपनी गोद में लिये कभी उसे दुलारता है तो कभी खुद रोने लगता है. पिता को बच्चे की लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है लेकिन व्यवस्था के पास यह सुविधा नहीं है. मजबूर पिता के पास एम्बुलेंस का किराया देने लायक पैसा नहीं. यह पहली बार नहीं हो रहा है. व्यवस्था निर्मम होती है इसलिए यह दृश्य आम है. व्यवस्था से शिकायत करना फिजूल है लेकिन लोगों की संवेदना का एक सोता भी उस मजबूर परिवार के लिए नहीं फूटा, यह अफसोसजनक है. किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया लेकिन हादसे की निर्ममता पर संवेदनाओं की नहर निकल पड़ी है. उस मजबूर परिवार को तो यह भी पता नहीं होगा कि वो कौन लोग हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं और उसे तो यह भी नहीं मालूम होगा कि यह सोशल मीडिया क्या बला है? इस पीड़ा पर सयापा करना भी एक तरह की हिंसा है क्योंकि जिनके हाथ मदद के लिए नहीं उठे, उन्हें क्या हक है कि वे उस दर्द पर आंसू बहाये. यह समय कठिन है और निर्मम भी. आभाषी दुनिया ने जैसे संवेदनाओं को निगल लिया है. ऐसे दर्जनों घटनायें आए दिन नुमाया होती हैं और हर घटना के साथ हम उसे बिसरा कर नयी घटना के लिए व्यवस्था को दोष देने निकल पड़ते हैं. व्यवस्था जिसे आप प्रबंधन भी कह सकते हैं, वह निर्मम है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन यह भी तय है कि मदद करने उसी व्यवस्था से ही कोई आगे आता है. क्या इस सच से आंख चुरा लेंगे?
मनोज कुमार/ सोशल मीडिया पर एक पीड़ादायक तस्वीर के साथ एक सूचना शेयर की जा रही है कि एक मजबूर पिता और एक मासूम बच्चा अपने भाई की लाश अपनी गोद में लिये कभी उसे दुलारता है तो कभी खुद रोने लगता है. पिता को बच्चे की लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत है लेकिन व्यवस्था के पास यह सुविधा नहीं है. मजबूर पिता के पास एम्बुलेंस का किराया देने लायक पैसा नहीं. यह पहली बार नहीं हो रहा है. व्यवस्था निर्मम होती है इसलिए यह दृश्य आम है. व्यवस्था से शिकायत करना फिजूल है लेकिन लोगों की संवेदना का एक सोता भी उस मजबूर परिवार के लिए नहीं फूटा, यह अफसोसजनक है. किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया लेकिन हादसे की निर्ममता पर संवेदनाओं की नहर निकल पड़ी है. उस मजबूर परिवार को तो यह भी पता नहीं होगा कि वो कौन लोग हैं, जो उनसे हमदर्दी रखते हैं और उसे तो यह भी नहीं मालूम होगा कि यह सोशल मीडिया क्या बला है? इस पीड़ा पर सयापा करना भी एक तरह की हिंसा है क्योंकि जिनके हाथ मदद के लिए नहीं उठे, उन्हें क्या हक है कि वे उस दर्द पर आंसू बहाये. यह समय कठिन है और निर्मम भी. आभाषी दुनिया ने जैसे संवेदनाओं को निगल लिया है. ऐसे दर्जनों घटनायें आए दिन नुमाया होती हैं और हर घटना के साथ हम उसे बिसरा कर नयी घटना के लिए व्यवस्था को दोष देने निकल पड़ते हैं. व्यवस्था जिसे आप प्रबंधन भी कह सकते हैं, वह निर्मम है, इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन यह भी तय है कि मदद करने उसी व्यवस्था से ही कोई आगे आता है. क्या इस सच से आंख चुरा लेंगे?
संवेदना शून्य होते समाज में हम मूल्य को खो चुके हैं. संवेदनाओं के पंख कुतर दिये गए हैं. मैं और मैं वर्तमान समय की पहचान बनकर रह गया है. कोविड के दरम्यान संवेदनाओं के झरने फूट पड़े थे. लग रहा था कि हमारे भीतर संवेदनाएं जाग उठी है. हमने दुबारा लोभ, लालच और ईष्र्या को धता बताकर मनुष्यता को प्राप्त कर लिया है लेकिन समय गुजरने के साथ सबकुछ बेमानी हो गया. पहले से ज्यादा और ज्यादा निष्ठुर हो गए. पराये तो छोडिय़े, अपने भी पराये हो गए. सांसें बच्चे की टूटे या पत्नी की लेकिन फिकर खुद की रह गई. ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई. कोविड को पराजित कर खड़े हो गए थे लेकिन खड़े मन के भीतर संवेदना मर चुकी थी. उनका कहना था कि अब अपने लिये सोचने का वक्त आ गया है. याद आता है कि जब संवेदना मर जाती थी तो बड़े लोग कहते थे कि एक बार श्मशान का फेरा लगा आओ. जिंदगी समझ आ जाएगी लेकिन आज जब मौत से जंग कर जो लौटे हैं, उनकी संवदेना खुद के लिए रह गयी है. श्मसान की सचाई भी उन्हें नहीं डराती है.
इस सब कड़ुवे सच के बीच एक सच यह भी है कि सबकुछ खत्म नहीं हुआ है. अभी बहुत कुछ बाकि है. संवेदना भी, आंसू भी और दूसरों के लिए दर्द भी. यह बाकि रह जाएगा. संवेदनायें बची रहेंगी लेकिन शर्त है कि आप संवाद करें. पिता-पुत्र के मध्य संवाद नहीं है, पति और पत्नी में अनबन नया नहीं है. हम अपना ही दर्द नहीं समझ पाते हैं तो दूसरों का दर्द क्या जानें. अब वक्त आ गया है कि हम एक-दूसरे से बात करें. भावनाओं को समझें और यह समझ संवाद से शुरू होगा. कम्युनिकेशन गैप संवेदनाओं के खत्म होने की प्रथम सीढ़ी है. कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले सिद्धांत पढ़ा रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो, यह बताने का गुर उन्हें भी पता नहीं है. कम्युनिकेशन का भारतीय परम्परा है पशु-पक्षियों से बात करना, चींटी के जीवन की रक्षा करना. पेड़-पौधों से बतियाना लेकिन हम अपनों से नहीं बतिया पा रहे हैं तो इन बेजुबानों से कौन बतियाये. जीवन में पूर्णविराम नहीं लगा है लेकिन अर्धविराम जरूर लग गया है. इस चिंह को पहचान लेंगे तो संवाद शुरू हो जाएगा. जरूरी है कि हम संकट में समाधान तलाश करें ना कि अवसर. इस अवसरवादिता ने ही तो हमारा बेड़ागर्क किया है. गुरु पूर्णिमा मनाइए लेकिन गुरु का कहा भी मानिये कि पहली रोटी गाय को दीजिये. यह परम्परा संवेदनाओं की जड़ों को सींचती है और हमें संवेदना शून्य होने से बचाती हैं. समय आ गया है कि आभाषी दुनिया में रोना रोने के बजाय धडक़नों को पहचानें और जिंदगी में एक नयी सुबह की शुरूआत करें.