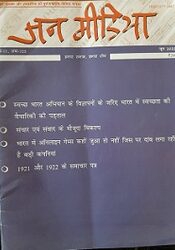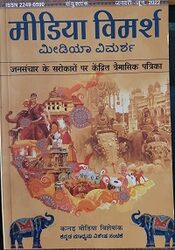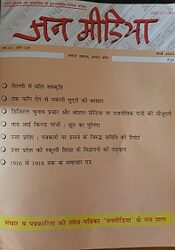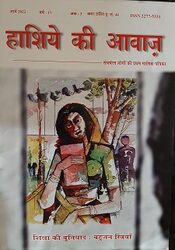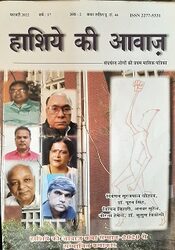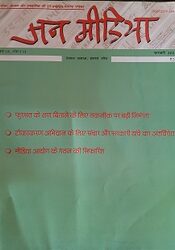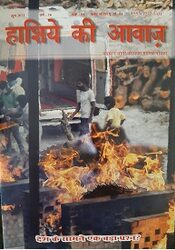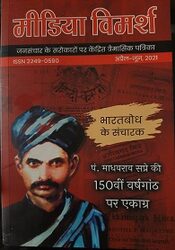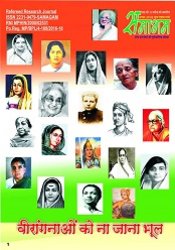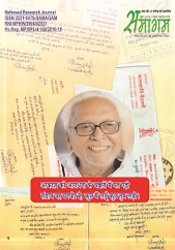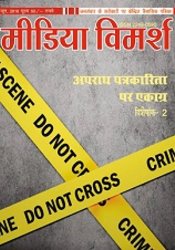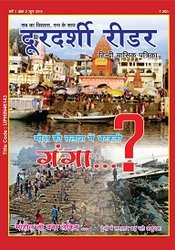एक था अखबार ( खण्ड-दो)
एक था अखबार ( खण्ड-दो)
दिनेश चौधरी/ जिस अखबार के दफ़्तर में चौबीसों घण्टे कर्फ्यू लगा रहता था और जहाँ घड़ी की टिक-टिक साफ सुनाई पड़ती थी, मुझे बतौर प्रशिक्षु 'पाठकों के पत्र' एडिट करने का जिम्मा दिया गया। साथ में सम्पादकीय पृष्ठ की कुछ सामग्री और कुछ साप्ताहिक परिशिष्ट। 'पाठकों के पत्र' वाला कॉलम तब बहुत लोकप्रिय होता था और शायद सबसे ज्यादा पढा जाता था।अखबार में कोई चूक हो जाए तो कई पाठक खटाक से पत्र लिख मारते थे, जो न केवल छपते थे बल्कि कई बार सम्पादक को भी कैफियत देनी पड़ती थी। ये अखबार की अघोषित नीति होती थी। तब की लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका 'सारिका' ने तो इस तरह के पत्रों के लिए 'ऐसे भी खत आते हैं शीर्षक से एक स्तम्भ ही बना लिया था। उदयन शर्मा की 'रविवार' इस मामले में कुछ ज्यादा ही उदार थी और स्वयं को दी जाने वाली गालियां भी श्रद्धा और सम्मान के साथ छापती थी। डूबने से पहले रविवार ने जब 'डेबोनायर' शैली की तस्वीरें छापना शुरू कर दीं तो एक पाठक ने टिप्पणी की, 'रविवार का स्तनांक प्राप्त हुआ..।' एक लेख पर एक अन्य पाठक की टिप्पणी थी, ''पूरा लेख एक बिके हुए दयनीय कुत्ते की कूँ-कूँ सा लगा पर लिखते हुए लोहिया प्रेत दिख रहा होगा इसलिए खुलकर कांय भी नहीं कर सका है। हाँ..... नाम के कुत्ते के गले में मोटी हड्डी दी गई है.. पत्र को छाप सको तो छाप लेना अन्यथा बत्ती बनाकर उचित इस्तेमाल कर लेना।" लिहाजा रविवार के सम्पादक- मंडल ने पत्र को छापने का ही विकल्प चुना और इसी पत्र के कारण रविवार की बहुत-सी प्रतियां बिकीं। कई तो मुझसे ही मांग कर ले गए और एक मित्र के पास से वापस आ जाती तो यह ऐतिहासिक दस्तावेज मैं आपके अवलोकनार्थ रख पाता।
तब इस कॉलम के जरिए सबसे आखिरी आदमी भी अपने मन की बात कह सकता था। गाँधी बाबा इस आखिरी आदमी का लिहाज करने पर खूब जोर देते थे। अब गाँधी बाबा का ही लिहाज नहीं रहा तो आखिरी आदमी का कहाँ से रहे? लिहाजा, बहुत से अखबारों ने पाठकों के पत्र वाला कॉलम बन्द कर दिया। सम्पादक-पाठक के बीच जो सम्वाद दोतरफा था वह एकतरफा हो गया और यह एक तरह की सेल्फी या आत्मरति है जो आत्ममुग्ध लोगों में लाइलाज बीमारी की तरह पायी जाती है। एक 'बड़े' अखबार के सम्पादक, जिन्होंने पाठकों के पत्र छापना बन्द कर दिया, खुद अपना सम्पादकीय बड़ा-लम्बा चौड़ा और प्रवचन के शिल्प में लिखते हैं जो मुझे निहायत अश्लील और उबकाई से भरा हुआ लगता है। एक बार मैंने अपने एक वरिष्ठ और अग्रज पत्रकार साथी से लम्बे-लम्बे प्रवचनों की गुणवत्ता पर सवाल किया तो उन्होंने थोड़े भदेस तरीके से कहा कि, 'जब गू पतला होता है तो वह ज्यादा फैलता है!'
बहरहाल, 'पाठकों के पत्र' वाले कॉलम की जिम्मेदारी मिलने से कस्बे में अपना रुतबा जरा बढ़ गया था और कुछ नमस्ते वगैरह भी होने लगी थी। नमस्ते करने वालों में कुछ छपास रोग से पीड़ित कवि भी थे, जो चाहते थे कि मैं कम से कम इसी कॉलम में उनकी कविताएं लगा दिया करूँ। एक सज्जन तो पूरा संग्रह ही सौंप गए थे, पर मुझे अपनी सीमाएँ पता थीं और जब मैंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया तो वे कस्बे में यह कहते घूमते पाए गए कि 'कल का छोकरा अपने को बड़ा पत्रकार समझने लगा है।' हालांकि यह बात सिर्फ अपन जानते थे कि अपनी हैसियत किसी बंधुआ मजदूर से ज्यादा नहीं है पर 'चौथे खम्भे' की गौरवशाली परम्परा और महान पत्रकारीय दायित्व के बोझ तले बुरी तरह से दबे होने के कारण अपन किसी को यह बात कह भी नहीं सकते थे। पत्रकार जितना अपने वेतन को लेकर चिंतित होते हैं, उससे ज्यादा उसे छुपाने को लेकर।
तो एक बार हुआ यूँ कि बस्तर के किसी कस्बे से एक पत्र आया कि आवासीय इलाके में एक शराबखाना खुलने से स्थानीय नागरिकों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन इसे अन्यत्र स्थानांतरित करे। यह सहज, सरल, वाजिब-सा पत्र था, इसलिए ज्यों का त्यों छप गया। इसके कुछ दिनों बाद दो रंगदार किस्म के व्यक्ति अखबार के दफ्तर में नमूदार हुए। 'पाठकों के पत्र वाले सम्पादक जी' का पता पूछते हुए ऐन मेरे सामने खड़े हुए और कहा कि अमुक नगर की दारूभट्टी के बारे में जो चिठ्टी आपने छापी है उसमें कोई दम नहीं है और कुछ लोग फकत ठेकेदार साहब को ब्लैक-मेल करना चाहते हैं जबकि ठेकेदार साहब गऊ किस्म के आदमी हैं और सुबह के अलावा शाम को भी सिर्फ गाय का दूध ही पीते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पत्र का खंडन छाप दूँ और इसके एवज में जो भी उचित शुल्क हो वह ग्रहण कर लूँ। मैंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया और कहा कि आपका जो भी पक्ष हो लिखकर भेज दें, छाप दिया जाएगा। ठीक है कहते हुए दूसरे रंगदार ने मेरे समक्ष बापू की तस्वीर वाला अनुशंसा पत्र रख दिया, जिसका मूल्य मेरे एक महीने के वेतन से दोगुना था। इस अप्रत्याशित हरकत पर मैं लगभग चीख पड़ा और सबने चौंक कर हमारी ओर देखा। जिस दफ्तर में बोलने-बतियाने की आवाज सुनाई न पड़ती हो वहां एक घुटी हुई चीख का निकल जाना भी बड़ी बात थी। सहकर्मियों ने चौंक कर हमारी ओर देखा और मधुशाला प्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया।
दोपहर को घर से लाए सब्जी-पराठे हम दफ्तर के बगल में एक होटल में खाते थे। होटल चलती हुई-सी थी, पर हम लोग अपने 'पत्रकार' होने के विशेषाधिकार का लाभ उठा लेते थे। फिर भी एक व्यस्त होटल में देर तक एक टेबल को घेरे रखने के अपराध-बोध से मुक्त होने और काउन्टर के सामने से हाथ हिलाते हुए गुजर जाने की शर्मिंदगी से बचने के लिए हम आखिर में आधी-आधी प्याली चाय मंगा लेते। उस दिन की चाय में हमारे साथ कप्पू जी ने भी हिस्सेदारी की और यह मेरा उनसे पहला परिचय था। मैंने उनसे हाथ मिलाया और जब बाद में पता चला कि ये परसाई जी के बड़े भक्त हैं तो मुझे कई दिनों तक अफसोस होता रहा कि मैं उनसे गले क्यों नहीं मिला? बहरहाल, कप्पू जी ने मुझे समझाया कि मुझे इतनी-सी बात पर इतना ओवर-रिएक्ट नहीं करना था। वे सिस्टम के मारे होंगे। आजकल सब जगह काम इसी तरह होता है तो उन्होंने यहाँ भी यही समझा होगा।
यही कप्पूजी एक दिन अपने झोले में टेबल घड़ी लेकर आए और उसे अपने सामने डेस्क पर रख दिया। थोड़ी पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि सम्पादक जी ने समय पर आने को लेकर कोई टोका-टाकी की है, इसलिए वे घड़ी साथ लेते आए, इस नारे के साथ कि, 'टाइम पर आना और टाइम पर जाना।' बावजूद इसके कि दफ्तर की घड़ी हस्बे-मामूल अपनी जगह पर टँगी हुई थी और वैसे ही टिक-टिक करती थी।
दफ्तर के बाहर कोई नया आदमी मिलता और उनसे पूछता कि आप क्या करते हैं, तो वे कहते कि ' जनाब! हम रद्दी बेचने का काम करते हैं!' मैं पत्रकारिता में नया था- पत्रकारिता के गौरव-भार से लदा हुआ। मुझे बुरा लगता। मुझे लगता कि वे पत्रकारिता के 'पवित्र' पेशे को बदनाम कर रहे हैं। उनसे शिकायत करता तो वे सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाते।
फिर अखबारों के धंधे में बड़ी पूँजी का आगमन हुआ। यह 2002-03 के आस-पास की बात होगी। मैंने गाजियाबाद में लंबे समय तक यूनियन के दफ्तर में डेरा डाला हुआ था। यहाँ 'हिंदुस्तान टाइम्स' आता था। मेट्रो सिटी के अपने-अपने अखबार हैं। मुम्बई का 'टाइम्स ऑफ इंडिया' है, कोलकाता का ' द टेलीग्राफ' और चेन्नई का 'द हिन्दू'। मैं कुछ गलत कह रहा होऊँ, तो कृपया मुझे टोक दें। तो जब 'एचटी' के इलाके में 'टीओआई' आया तो बड़ी मार-काट मची। अखबार के दाम घटकर केवल एक रुपये हो गए और पन्नों का बोझ बढ़ गया। हॉकर बेचारा दुखी था। एक दिन कहा कि , 'बाबूजी, ग्राहक बनाए रखने की मजबूरी है, वरना पेपर को रद्दी के भाव बेच दें तो इससे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे।'
उस दिन मैंने अखबार नहीं पढ़ा। सारा दिन कप्पू जी को याद करता रहा।
(दिनेश जी के फेसबुक वाल से साभार)