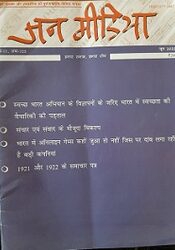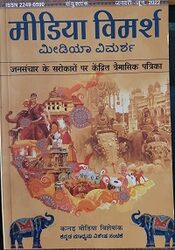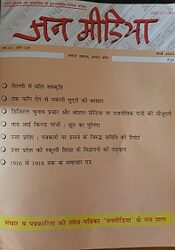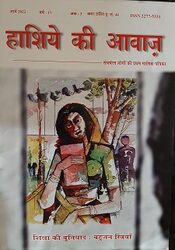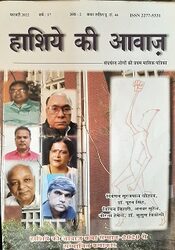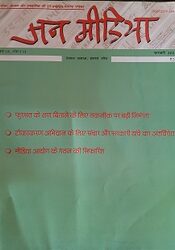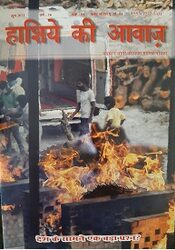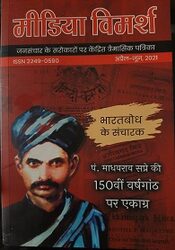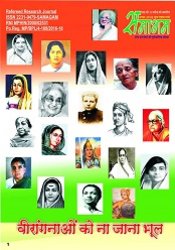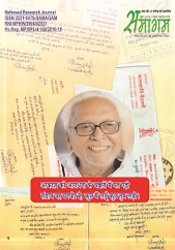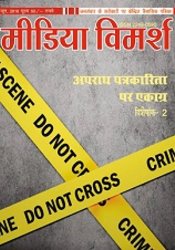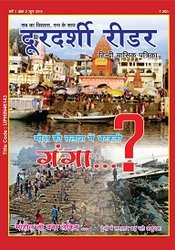फिर से नए रूप में
फिर से नए रूप में
नब्बे के दशक में यह एक शोध पुस्तक की शृंखला में प्रकाशित हुई थी .जिसमें लालू यादव पर अंबरीश कुमार ने लिखा .तब लालू की धमक भी थी .इस पुस्तक का तब वीपी सिंह को विमोचन करना था पर अचानक उनकी तबियत बिगड़ने पर मुख्य अतिथि कांशीराम ने इसका और अन्य पुस्तकों का विमोचन किया .अब इसे फिर से नए रूप में ई बुक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है .इसकी मुख्य भूमिका अरुण कुमार त्रिपाठी और प्रभात खबर के संपादक रहे राजेन्द्र तिवारी ने लिखी है .यह जीवनी नहीं एक अध्ययन है . आवरण चंचल का है। इस पुस्तक की भूमिका -------------
प्रतिक्रांति से परास्त लालू प्रसाद
लालू प्रसाद यादव का पतन और पराभव किसी एक राजनेता के पतन की परिघटना नहीं है। यह सामाजिक क्रांति और धर्मनिरपेक्षता की पराजय है और प्रतिक्रांति की विजय है। लालू प्रसाद पर लिखना और उनकी राजनीति का तटस्थ विश्लेषण करना आसान नहीं है। या तो लोग कोसते कोसते उन्हें गयासुर राक्षस जैसा बना देते हैं या फिर उनकी प्रशंसा करते करते उन्हें श्रीकृष्ण का दर्जा दे दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अक्सर कहा करते थे कि हमें या तो देवता चाहिए या दैत्य। हमें मनुष्य नहीं चाहिए। लालू प्रसाद उसी भारतीय मानस के शिकार हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे दूध के धुले हैं और उनका दोष नहीं है लेकिन सिर्फ उन्हीं पर सारा दोष मढ़ देने से हम उस व्यापक परिघटना से अनभिज्ञ रह जाते हैं जो भारतीय समाज में हजारों साल से चल रही है और आगे भी वह चलती रहने वाली है। इस परिघटना या प्रवृत्ति को स्वामी धर्मतीर्थ ने अपनी पुस्तक ` हिस्ट्री आफ हिंदू इम्पीरियलिज्म ’ में भारतीय जाति व्यवस्था के विशिष्ट चरित्र से जोड़ा है। उनका कहना है कि हजारों सालों से वर्णव्यवस्था और उसे मदद करने वाली जाति व्यवस्था को तोड़ने की कोशिशें किसी न किसी साजिश का शिकार होती रही हैं। वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर बैठी शक्तियां अपनी चालाकियों से ऐसी योजना बनाती हैं कि उसे कमजोर करने वाली ताकतें अक्सर हार जाती हैं।
नब्बे के दशक में जब मंडल आयोग की रपट के बहाने उत्तर भारत में एक जबरदस्त सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई उसी समय अयोध्या में मंदिर निर्माण के बहाने प्रतिक्रांति अपना तानाबाना बुन रही थी। नब्बे का दशक दोनों के बीच जबरदस्त टकराव का कालखंड माना जाएगा। उनके बीच वैश्वीकरण और उदारीकरण के बहाने एक समझौता होता है लेकिन 2014 तक आते आते प्रतिक्रांति जीत जाती है और सामाजिक क्रांति हार जाती है। ऐसा नहीं कि सामाजिक क्रांति लालू प्रसाद के साथ ही शुरू हुई और उनके पराभव के साथ ही समाप्त हो जाएगी। पर उत्तर भारत में सामाजिक क्रांति की जो प्रक्रिया अस्सी के दशक में आरंभ हुई और नब्बे के दशक में परवान चढ़ी उसमें लालू प्रसाद एक शिखर को छूते हुए नजर आते हैं। उस प्रक्रिया को तेज करने में अगर कांशीराम का योगदान है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी योगदान कम नहीं है। उसे रामविलास पासवान और शरद यादव ने अपने ढंग से बढ़ाया तो मुलायम सिंह यादव ने उसे अलग मजबूती प्रदान की। इस प्रक्रिया का आधुनिक इतिहास कर्पूरी ठाकुर से होते हुए राम मनोहर लोहिया, डा भीमराव आंबेडकर, ज्योतिबा राव फुले, पेरियार, अन्नादुराई, करुणानिधि और नारायण गुरु तक जाता है। मध्ययुग के भक्ति आंदोलन में कबीर, रैदास, दादू और चोखामेला के रूप में हम इसका आध्यात्मिक रूप देखते हैं।
पिछली सदी में भारत की जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा झटका डा भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी के प्रयासों से लगा। हालांकि ऊपरी तौर पर दोनों राजनेताओं में एक टकराव दिखाई पड़ता है और उस टकराव का प्रतिफल 1932 के पूना समझौते के रूप में आता है। आंबेडकर जहां जाति व्यवस्था के समूल नाश की बात करते हैं वहीं गांधी उसे ढीला करने के प्रयास में लगे हैं। वे पहले छुआछूत खत्म करने पर जोर देते हैं और तब वर्णव्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं लेकिन बाद में गांधी कहते हैं कि वे सिर्फ एक वर्ण में यकीन करते हैं। अंतिम दिनों में गांधी सिर्फ उसी शादी में जाते हैं जहां अंतरजातीय विवाह होता है। आंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने वाली दलित राजनीति गांधी को चाहे जितना सवर्णवादी सिद्ध करे लेकिन भारत के ज्ञात इतिहास में जाति व्यवस्था को इतने व्यापक रूप से किसी एक आदमी ने अगर झटका दिया तो वह गांधी ही थे। येरवदा जेल में महात्मा गांधी के अनशन के बाद तमाम मंदिरों के दरवाजे दलित जातियों के लिए खोल दिए गए थे। लेकिन कट्टर सवर्ण समाज गांधी के इस अभियान से खुश नहीं था। इसीलिए जब 1933 में जेल से बाहर निकलने के बाद वे छुआछूत निवारण यात्रा पर निकलते हैं तो पुणे में उनके काफिले पर बम से हमला होता है जिसमें उनके कुछ साथी घायल होते हैं। यह भी सर्वविदित है कि गांधी की हत्या के कारणों में एक कारण यह भी था कि उन्होंने हिंदू समाज के वर्ण आधारित ढांचे को कमजोर करने का प्रयास किया था। यह संयोग नहीं है कि गांधी पर हमला करने वाले और उनकी हत्या करने वाले संगठनों और व्यक्तियों का संबंध महाराष्ट्र और पुणे के कट्टर हिंदू संगठनों से है और लालू प्रसाद को परास्त करके जेल भिजवाने वालों के तार भी वहां से जुड़ते हैं।
इसलिए लालू प्रसाद के पराभव और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों में सजा दिलवाने के पीछे उस वर्णवादी आक्रोश को खारिज नहीं किया जा सकता जो बिहार ही नहीं भारत के सवर्ण समाज के भीतर उनके विरुद्ध उबल रहा था। लालू प्रसाद ने अपने संवाद और शासन की भदेस शैली बिहार के सवर्ण समाज को हिला दिया था। उन्होंने पिछड़ों और दलितों में नए किस्म का आत्मविश्वास भरा था और अल्पसंख्कों को सुरक्षा की गारंटी दी थी। लालू इस वर्णव्यवस्था से जिन हथियारों से लड़ रहे थे उनमें एक था सामाजिक न्याय और दूसरा था धर्मनिरपेक्षता। उनके विरुद्ध सवर्णों के गुस्से को केंद्र में रखकर हिंदुत्ववादी शक्तियां जिन हथियारों से लड़ रही थीं उनमें एक था भ्रष्टाचार विरोध और दूसरा था राष्ट्रवाद। लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के आरोप का मुकाबला अपने जातीय आधार से कर रहे थे और राष्ट्रवाद का मुकाबला धर्मनिरपेक्षता केंद्रित उदार देशभक्ति से। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद और उनके प्रतिद्वंद्वी नीतीश कुमार और सुशील मोदी और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा(पूर्व जनसंघ) जयप्रकाश नारायण के उस आंदोलन में शामिल थे जो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरुद्ध खड़ा हुआ था। इसलिए आज की भाजपा को उसी डंडे से लालू प्रसाद को पीटने में सुविधा हुई और उसने उन्हें परास्त कर दिया। लेकिन यह बात जरूर ध्यान देने की है कि जेपी आंदोलन में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम नहीं था और न ही मंदिर बनाने और 370 हटाने की मांग थी। यह लालू प्रसाद की विफलता रही कि वे जेपी आंदोलन की उस विरासत का स्मरण नहीं दिला पाए जिसका लक्ष्य संपूर्ण क्रांति था और जिसके इर्द गिर्द भाजपा कहीं नहीं है। दरअसल लालू प्रसाद ने भी उन आदर्शों को त्याग दिया था और यही वजह है कि उनके भीतर वह नैतिक शक्ति नहीं बची जिसके बूते पर वे भाजपा के हिंदुत्व से लड़ सकते।
लालू प्रसाद की पूरी योजना सामाजिक न्याय को एक लोकप्रिय रणनीतिक हथियार बनाते हुए कांग्रेस की भ्रष्ट और धर्मनिरपेक्ष काया के साथ गठजोड़ कायम करना था। उन्होंने कांग्रेस की तरह ही अपनी पार्टी पर परिवार को बिठा दिया, उसे भ्रष्ट हो जाने दिया। लालू ने इतना जरूर किया कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता को सामाजिक न्याय के साथ मिलाकर उसका एक व्यावहारिक स्वरूप निर्मित किया। कांग्रेस अगर सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यकों का गठजोड़ बनाकर पूरे देश पर एक उदार और धर्मनिरपेक्ष दायरे में शासन करती थी तो लालू प्रसाद ने उस समीकरण में से सवर्णों को हटाकर उसमें अल्पसंख्यकों के साथ पिछड़ों को आक्रामक तरीके से जोड़ दिया। अगर मुलायम सिंह ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने की कोशिश कर रहे कारसेवकों पर गोली चलवा कर तो लालू प्रसाद ने रथयात्रा पर निकले लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके अल्पसंख्यकों में अपना स्थायी वोटबैंक बनाया तो कांग्रेस ने अपने शासन काल में राममंदिर का शिलान्यास कराकर और बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने का मौका देकर अल्पसंख्यकों का वोट गंवा दिया।
नब्बे के दशक में हुई भारतीय राजनीति की इस जबरदस्त उथल पुथल के बीच लालू प्रसाद और मुलायम सिंह धर्म निरपेक्ष राजनीति के आधार स्तंभ बन गए। उस समय तेजी से उठते हिंदुत्व के ज्वार से भयभीत लोग जब बौद्धिकों से यह सवाल करते थे कि भारत के धर्मनिरेपक्ष ताने बाने और संविधान का क्या होगा तो जवाब मिलता था कि भारत और विशेषकर उत्तर भारत की जातीय संरचना की विविधता उसे बचा लेगी। कुछ लोग तो क्रूर शब्दों में कहते थे कि हिंदुत्व को क्या भारत की जाति व्यवस्था रोक नहीं लेगी। यह आत्म विश्वास इस देश के बौद्धिकों और विशेषकर कांग्रेस प्रणाली में यकीन करने वालों को आक्रामक धर्मनिरपेक्षता का कोई आख्यान खड़ा करने ही नहीं देता था। उन्होंने लालू और मुलायम को धर्मनिरपेक्षता की गारंटी का जिम्मा दे रखा था और मानते थे कि अन्य क्षेत्रीय दल सहज रूप से इन सबसे जुड़ जाएंगे और भारतीय राजनीति और समाज के उदार और सेक्यूलर ढांचे को बचा लिया जाएगा।
पिछले दिनों एक समाजवादी मित्र ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने परिवार को बचा लिया। इस तारीफ में परोक्ष रूप से यह भाव छिपा हुआ था कि लालू प्रसाद नहीं बचा पाए। इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बलि चढ़ाकर अपने परिवार को बचा लिया जबकि लालू प्रसाद ने धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर समझौता करने से इनकार करके अपना और पार्टी का बंटाधार कर लिया। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद के पराभव के लिए उनका अहंकार, भ्रष्ट चरित्र और परिवारवाद जैसी कमजोरियां तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन उन सबको बढ़ाचढ़ाकर पेश करने और उनकी छवि और राजनीति का नाश करने में हिंदुत्ववादी शक्तियों की बड़ी योजना दिखाई पड़ती है। लेकिन लालू के पराभव के पीछे सामाजिक न्याय की शक्तियों का अंतर्विरोध और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी कम दोषी नहीं है। लालू अगर देवगौड़ा से न टकराए होते तो उन पर सीबीआई के निदेशक जोगिंदर सिंह इतनी कड़ी जांच न करते, अगर वे पासवान और नीतीश को मिलाकर चलते तो इतने कमजोर न होते और आखिर में अगर उनका और मुलायम सिंह का साथ रहा होता तो समाजवाद को लाने और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने का आंदोलन इतना कमजोर न होता।
समाजवादी आंदोलन के बिखराव की इस प्रक्रिया को कुछ सवर्ण नेता दूसरे तरीके से पेश करते हैं। उनका कहना है कि अगर मंडल से निकली ताकतें चरित्रवान होतीं तो भारतीय राजनीति का न तो सांप्रदायीकरण हुआ होता और न ही उसके सामने फासीवाद का खतरा खड़ा होता। यह बात ध्यान देने की है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादियों की व्यापक एकता का प्रयास हुआ था और मुलायम सिंह के नेतृत्व में एक पार्टी बनाने का फैसला किया गया। लेकिन मुलायम सिंह के परिवार की आपसी खींचतान के चलते वह एकता नहीं हो पाई और बाद में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ बिहार में अपने उम्मीदवार खड़े किए बल्कि विपक्ष के गठबंधन के विपक्ष में खुलकर प्रचार भी किया। समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 2015 के चुनाव में लालू और नीतीश के गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया।
यह हैरानी की बात नहीं है कि आजकल जेल में पड़े समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उस समय इस बात का तेजी से प्रचार शुरू कर दिया था बिहार ने रास्ता दिखा दिया है और देश को उस पर चलना चाहिए। उनका संकेत गैर कांग्रेसवाद की रणनीति को विलीन करने और गैरभाजपा की रणनीति पर काम करने का था। लेकिन 2017 में लालू प्रसाद को सजा होने और उन्हें स्थायी रूप से जेल भेजे जाने और उन पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लग जाने के बाद सारी बाजी पलट गई। चार साल पहले मोदी को सांप्रदायिक बताकर जो नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे उन्होंने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया और लालू प्रसाद ने गैरभाजपावाद की जो रणनीति बनाई थी वह ऐसी विफल हुई कि 2019 में केंद्र में भाजपा और ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में आ गई। यह घटनाक्रम गैरभाजपावाद को करारा झटका तो था ही उन लोगों के लिए सबक था जो भाजपा और मोदी का विकल्प बनने का स्वप्न देख रहे थे। उसी कड़ी में बिहार के रास्ते को आदर्श बताने वाले आजम खान के भी जेल जाने को देखा जा सकता है।
लालू प्रसाद की खूबी यही है कि उन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को खत्म जरूर किया लेकिन बाद में गैरकांग्रेसवाद की रणनीति को भी छोड़ दिया। वे वैचारिक रूप से गतिशील रहे और राजनीतिक रूप से करेक्ट। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता गैरभाजपावाद को एक रणनीति के रूप में विकसित करना है जो इस समय की सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष राजनीति की सबसे बड़ी मांग हो सकती है। इसके जवाब में भाजपा की ताकत यह रही है कि उसने सामाजिक न्याय की शक्तियों का हिंदूकरण किया और गैरकांग्रेसवाद की रणनीति को एक सिद्धांत का रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के साथ भाजपा ने उन क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लाने में पूरी ताकत झोंक दी जो भारत की नई लोकतांत्रिक राजनीति के प्राणतत्व थे। लालू प्रसाद की दिक्कत यह रही कि वे अपनी निरंतर बिगड़ती छवि के कारण न तो क्षेत्रीय दलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन पाए और न ही गैरभाजपाई दलों के लिए। बिहार तक सीमित उनकी पार्टी का आकर्षण अखिल भारतीय बन पाता इससे पहले वे बिखरने लगे। आज लालू प्रसाद की स्थिति चंद्रगुप्त बनने की तो नहीं ही बची लेकिन चाणक्य बनने के लिए भी जिस साख और मानसिक सक्रियता की जरूरत होती है वह भी वे खोते गए हैं।
पिछले साल लालू प्रसाद ने नलिन वर्मा के साथ मिलकर जेल से अपनी आत्मकथा तैयार की थी। उसका शीर्षक है—गोपालगंज टू रायसीना। वह पुस्तक कहती है कि लालू से उनके विरोधियों ने हमेशा नफरत की। लालू अपने बारे में कहते हैं कि वे हमेशा ईमानदार रहे हैं और गरीबों के लिए समर्पित हैं। लालू ने सेक्यूलरिज्म से कभी समझौता नहीं किया। वे भाजपा से नफरत करते हैं और कांग्रेस से प्रेम करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि बाद में इतिहास उनके साथ इतना क्रूर नहीं रहेगा जितना आज दिख रहा है। इस पुस्तक में लालू प्रसाद के बचपन की बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें गरीबी और संघर्ष साफ दिखता है। लालू की मां कहती थीं कि उन्हें एक भूत ने बचाया था। उनके बड़े भाई गुलाब राय को अजीब बीमारी थे जिसमें वे कई बार मरकर जी उठते थे। लालू यादव ने एक बार हींग का बोरा कुएं में फेंक दिया तो उनके पिता जी ने उन्हें पटना भेज दिया। वहां उनके भाई चपरासी थे जिनके पास लालू रहने लगे। पुस्तक लालू प्रसाद के अन्य समकालीनों सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार के बारे में बहुत कम बोलती है। इसमें लालू के छोटे बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पर दस पेज हैं। उसमें उनकी वक्तृत्व कला, सांगठनिक क्षमता और क्रिकेट प्रेम का भी वर्णन है। इसका आखिरी अध्याय लालू की भावनाओं को व्यक्त करता है। इस अध्याय का शीर्षक है---अभी तो मैं जवान हूं। उसमें कहा गया है कि मैं अस्पताल और जेल आता जाता रहा हूं। लेकिन इससे मुझे खारिज नहीं किया जा सकता। भविष्य शासक दल के नेताओं के हाथ में नहीं उस सर्वशक्तिमान के हाथ में है।
अंबरीश कुमार जो मेरे चालीस साल पुराने मित्र हैं उन्होंने पहली बार 1997 में यह पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में अंबरीश कुमार की राजनीतिक रिपोर्टिंग की मुहावरेदार शैली की छाप हर पन्ने पर मौजूद है। अंबरीश कुमार की भाषा सहज और सरल है और उनके प्रतीक सीधे जमीन से आते हैं। उनके लेखन पर जहां लोहिया की भाषा का प्रभाव है वहीं लालू की चुटकुला शैली भी दिखाई देती है। पुस्तक जब पहली बार आई तब लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे थे लेकिन उनका राजनीतिक सूर्य भी चमक रहा था। वे प्रधानमंत्री तय करते थे और यह भी निर्णय करते थे कि देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार कितने दिन चलानी और कब गिरानी है। पत्रकार और समाजशास्त्री अभय कुमार दुबे के मार्गदर्शन में तैयार की गई सात पुस्तकों में कल्याण सिंह और मेधा पाटकर का मोनाग्राफ मैंने लिखा था। मुलायम सिंह, कांशीराम और बाल ठाकरे पर अभय दुबे जी ने लिखा था और ज्योति बसु पर अरुण पांडे ने। यह श्रृंखला इस आशा के साथ तैयार की गई थी कि इसमें चुने गए नेता और उनकी राजनीतिक शैली आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा को तय करेगी। इन पुस्तकों का विमोचन बहुत रोचक वातावरण में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के आवास पर हुआ था। संयोग से उस समय वीपी सिंह को डायलसिस के लिए जाना पड़ा और कार्यक्रम में उनका संदेश पढ़ा गया। वह संदेश अंबरीश कुमार और अरुण पांडे लेकर पहुंचे थे। लेकिन कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति थी कांशीराम की। उनके अलावा प्रोफेसर रजनी कोठारी, राजेंद्र यादव और डा पुरुषोत्तम अग्रवाल भी उस समय मौजूद थे। कांशीराम उस कार्यक्रम विस्तार से बोले और उन्होंने भारतीय राजनीति में चल रही सामाजिक क्रांति की आवश्कता को रेखांकित किया। उससे पहले वे 1993 में मुलायम सिंह के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने और फिर भाजपा से मिलकर मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग कर चुके थे। लेकिन तब सामाजिक न्याय की शक्तियां हिंदुत्व से पराजित होने की स्थिति में नहीं थीं। बल्कि हिंदुत्व की शक्तियां अपनी विजय के लिए उनकी मुखापेक्षी थीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा लगातार पराभव की ओर जा रही थी और बिहार में भी उसका वैसा उभार नहीं हुआ था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा पांच साल बाद एक दूसरे से सत्ता बदल लेती थीं। दक्षिण के प्रवेश द्वार कर्नाटक में भाजपा को सत्तारूढ़ होने का मौका नहीं मिला था और पूर्वोत्तर के किसी राज्य में भाजपा को सत्ता नहीं मिल पाई थी।
लेकिन आज जब भाजपा और हिंदुत्ववादी शक्तियों का सूर्य उत्तरायण है और भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने की आहटें तेज हैं तब लालू प्रसाद का मोनाग्राफ फिर से प्रकाशित करना न सिर्फ साहस का विषय है बल्कि इतिहास के एक आवश्यक आख्यान का पुनर्पाठ भी है। आज लालू का नाम लेते ही सवर्ण समाज बिदक जाता है और पिछड़ा समाज भी खुलकर लालू के पक्ष में नहीं बोल पाता। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वह लालू के प्रेम का प्रतिदान दे सके लेकिन भाजपा इस स्थिति में जरूर है कि वह लालू को जमींदोज कर दे। आज जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है तब लालू प्रसाद एक बार फिर चर्चा में हैं। अमित शाह ने कोरोना संकट को भूलकर और जनता की तकलीफों को दरकिनार करके वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चुनाव का बिगुल बजा दिया है। नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान में लालू प्रसाद पर हमला किया है। उधर तेजस्वी यादव की तैयारी बहुत ढीली है। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में लालू का चुंबकीय व्यक्तित्व क्या कोई असर डाल पाएगा या नहीं यह देखा जाना है। इसके बावजूद लालू प्रसाद महज एक सजायाफ्ता राजनीतिक ही नहीं भारतीय समाज और राजनीति की एक परिघटना भी हैं। उन्हें खारिज करना परिवर्तन की राजनीति को खारिज करना है। उम्मीद है अंबरीश कुमार की पुस्तक के इस नए संस्करण से उस पुराने विमर्श की स्मृतियां कौंधेंगी और भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय मे यकीन करने वाली पार्टियों के बीच नए समीकरण का महत्त्व रेखांकित होगा।
अरुण कुमार त्रिपाठी, गाजियाबाद, 16 जून 2020.
बिहार और लालू
बिहार में सर्वकालिक सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल में बंद हैं। उन पर भ्रष्टाचार के और भी कई गंभीर मामले चल रहे हैं जिनमें फैसला आना अभी बाकी है। ठेठ देसी-बिहारी अंदाज वाले लालू प्रसाद ने १९९० के बाद बिहार के राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। उनकी राजनीति ने कांग्रेस को ऐसा उखाड़ा कि अब कांग्रेस को बिहार में बने रहने भर के लिए लालू प्रसाद की पार्टी की ही उंगली पकड़ कर चलना पड़ रहा है। और, भाजपा भी अपने बूते उतर कर बिहार की सत्ता हासिल करने की सोच नहीं पा रही। २००५ में ज्यादा विधायकों के बावजूद भाजपा को पिछड़े वर्ग से आने वाले नीतीश कुमार को नेता मानना पड़ा।
२०१५ का बिहार विधानसभा चुनाव सबको याद है। यानी १९९० से पहले तक राजनीतिक रूप से सवर्ण दबदबे वाले बिहार में पिछले ३० साल में सिर्फ चार मुख्यमंत्री हुए और चारों पिछड़े या दलित। २०१५ में जब भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में मिली भारी विजय के जोश बिहार विधानसभा के लिए उतरी तो उसे अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। यह लालू प्रसाद यादव का ही कमाल था। महागठबंधन की पहली सभा वैशाली जिले के एक गांव में थी जिसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, दोनों को शामिल होना था। पहले लालू प्रसाद आए और फिर नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के हावभाव में लालू प्रसाद के साथ दिखने का संकोच साफ झलक रहा था। लालू प्रसाद ने मंच पर नीतीश कुमार को गले लगाया और अपने अंदाज में कहा छोटा भाई है, सब माफ। संघ प्रमुख ने उस चुनाव के दौरान ही आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दिया था। यह बयान आया और लालू प्रसाद ने इसे ही मुद्दा बना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एमएस गोलवलकर की किताब जलाने की चुनौती दे डाली कि अगर आप अपने वादे के पक्के हैं तो अपने गुरु गोलवलकर की पुस्तक ‘बंच आफ थाट्स' को जला कर दिखाइये जिसमें पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करने पर जोर दिया गया है। चुनावी बाजी पलट चुकी थी। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में खुद को देश का पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री बताया, उस दिन शाम को लालू जी से बात हुई। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा कि पिछड़ी जाति से पहला प्रधानमंत्री तो आपने बनवाया था। लालू जी चौंक पड़े। उन्होंने तुरंत एचडी देवगौड़ा को फोन लगवाया और उनसे उनकी जाति की जानकारी ली। फोन बात करते-करते ही उन्होंने आवाज दी कि प्रेस व टीवी वालों को बुलाओ, अभी बात करनी है।
२०१५ के विधानसभा चुनाव बहुत से लोगों का कयास था कि लालू प्रसाद राजद की ज्यादा सीटें आने पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। नतीजे आए। राजद की जदयू से १० सीटें ज्यादा आईं। लेकिन एक बार भी लालू प्रसाद की ओर से ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे यह लगता कि वे नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहते। दरअसल, लालू प्रसाद व नीतीश कुमार में एक बड़ा अंतर यह भी है कि एक स्पष्ट वक्ता और मन का साफ है तो दूसरा पेट का गाढ़ा। यह चीज तब सामने भी आ गयी जब लालू प्रसाद के जेल जाने के साथ परिवार को भ्रष्टाचार के मामले में घेर कर दबाव बढ़ाना शुरू किया गया। नीतीश कुमार के सामने उस समय दो रास्ते थे। पहला रास्ता था लालू प्रसाद के दोनों बेटों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का। इस रास्ते पर अगर नीतीश कुमार चलते तो भी राजद को समर्थन जारी ही रखना पड़ता। लालू प्रसाद सरकार गिरने नहीं देते, ऐसा उनके कुछ करीबियों का मानना था। दूसरा रास्ता वह था जो नीतीश कुमार ने अपनाया। उनके इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही भाजपा समर्थन देने के लिए सामने आ गयी। इस बार भाजपा नीतीश कुमार की उन सभी बातों की धज्जियां उड़ाती रही जिनको हाशिये पर रखने के वादे के बाद जार्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार एनडीए में आए थे और जिनकी वजह से २०१३ में नीतीश कुमार ने एनडीए से किनारा किया था। इस तरह नीतीश कुमार सुशासन बाबू से सत्ता कुमार बन गये। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस लक्ष्य के साथ लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर आगे की राजनीति के लिए भरोसा किया, वह जमींदोज हो गया। नीतीश कुमार ने भाजपा से अंदर ही अंदर गोटी फिट करके पूरे राजद को ही भ्रष्ट करार देने की मंशा से इस्तीफा दिया था। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि राजद में शीर्ष नेताओं में यदि लालू प्रसाद के परिवार को छोड़ दें तो खांटी ईमानदार नेता ज्यादा निकलेंगे बनिस्पत जदयू के। जदयू में शीर्ष नेताओं में नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत रूप से कोई आरोप कभी नहीं लगा लेकिन उनके करीबी लोगों में से कई की जनता में छवि पैसा बनाने वालों की ही है।
लालू प्रसाद कैद में हैं और उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब है। उन्होंने २०१५ में ही अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौपने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी लेकिन जेल जाने की वजह से प्रक्रिया धरी रह गई और विरासत तेजस्वी यादव पर सवार हो गई। तीस साल बाद पहली बार ऐसा होगा, जब बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद मैदान में नहीं दिखेंगे। तेजस्वी यादव अब तक के अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाये हैं कि उनको लालू प्रसाद की विरासत को आगे ले जा सकने योग्य माना जा सके। २०२० के विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ तय होगा, देश और बिहार की राजनीति के लिए। ऐसे समय में वरिष्ठ पत्रकार अंबरीश कुमार की यह पुस्तक लालू प्रसाद के उन दिनों को समझने में महत्वपूर्ण होगी, जब वह अपने उरूज पर थे। और, साथ ही बिहार की राजनीति व उस मोड़ को भी समझने में सहायक होगी, जहां से बिहार ने मौजूदा राह पकड़ी थी।
राजेंद्र तिवारी
रांची 23 जून 2020