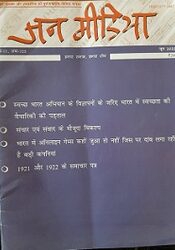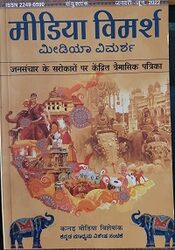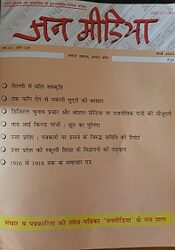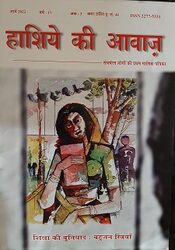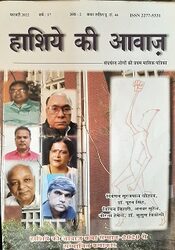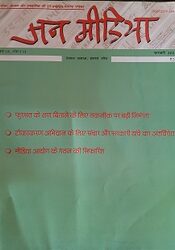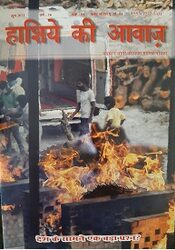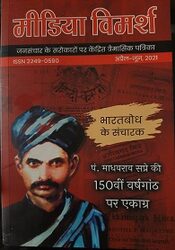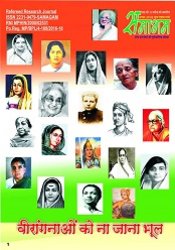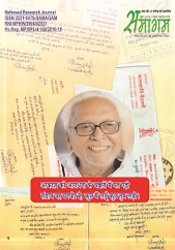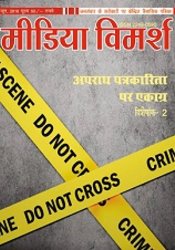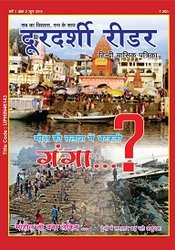अभिषेक दास/ भारतीय मीडिया के लिए यह संक्रमण का समय हैे। नव-पूँजीवाद की वर्तमान दौड़ में मीडिया की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं। खबरों के चयन से लेकर उसकी प्रस्तुति तक पर राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगाया जा रहा है। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया; कोई भी इस तरह के आरोपों से अछूता नहीं है।
अभिषेक दास/ भारतीय मीडिया के लिए यह संक्रमण का समय हैे। नव-पूँजीवाद की वर्तमान दौड़ में मीडिया की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठाये जा रहे हैं। खबरों के चयन से लेकर उसकी प्रस्तुति तक पर राजनीतिक पक्षधरता का आरोप लगाया जा रहा है। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया; कोई भी इस तरह के आरोपों से अछूता नहीं है।
दरसल, उद्धयोगीकृत हो चुके जनसंचार माध्यमों के लिए आज खबरें उत्पाद हैं। सूचनाएँ उसी रूप में परोसी जा रही हैं जो मीडिया घरानों के लिए पूँजी लाने में सहायक हो। और पूंजी के इसी प्रवाह को बनाए रखने के लिए मीडिया उद्योग का राजनीतिक दलों की ओर झुकाव होता चला जाता हैं। राजनीतिक दलों से ये नजदीकियाँ खबरों के स्वरूप को प्रभावित तो करती ही हैं, कभी-कभार मीडिया हाउसों को राजनीतिक दलों के एजेंडे को बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षां के दौरान देश में इस तरह की प्रवृृति में अप्रत्याशित वृृद्धि देखी जा सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में जनसंचार माध्यमों की किसी खास राजनीतिक दल के लिए प्रतितद्धता किसी भी दृृष्टि से सही नहीं ठहराई जा सकती है। लेकिन यह सवाल भी मौजूँ है कि आखिर वे कौन-सी मजबूरी है जिस कारण लोकतंत्र के चैथे स्तम्भ को अपना पुनर्संस्कार करना पड़ा ?
दरअसल जनसंचार माध्यमों के विकास का आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं से गहरा संबंध है। इस संदर्भ में मीडिया के विकास को इस रूप में देखा जा सकता है कि एक स्वतंत्र उद्योग के रूप में इसने किस हद तक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। और जब हम एक स्वतंत्र उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ भी वे सभी नियम लागू होंगे जो किसी अन्य व्यवसाय पर होते हैं। लेकिन अन्य व्यवसायों और मीडिया में अंतर होता है। मीडिया विचारों का भी उत्पाद करता है। कार्ल माक्र्स ने लिखा है कि- ‘‘भौतिक उत्पादन के साधनों पर जिस वर्ग का नियंत्रण होता है, उसी समय उसका बौद्धिक उत्पादन के साधनों पर भी अधिकार होता है।’’ यानि मीडिया पर नियंत्रण करने वाला वर्ग ही वैचारिक उत्पादों पर भी अपना अधिकार कायम करने का प्रयास करता है।
इस नजरिए से देखें तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ इस उद्योग पर से पूँजीवादी और साम्राज्यवादी नियंत्रण स्वतः समाप्त हो जाना चाहिए। कई बार तो इसी स्वरूप में सूचना और संचार के विकास को पेश भी किया जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि वर्Ÿामान परिप्रेक्ष्य में सभी संकेत इसके विपरीत ही दिखाई देते हैं। ऐसे विपरित संकेतों से कोई आश्चर्य भी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आज हम उस वैश्विक अर्थव्यवस्था निगम संकेन्द्रण सिद्धांत सिर्फ मुनाफे पर आधारित होता है। मीडिया घरानों को दस बात से कोई लेना-देना नहीं रह जाता है कि वे लोगों के सामने क्या परोस रहे हैं और उसका हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर असर होगा। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज ऐसा ही हो रहा है।
लोकतांत्रिक प्रणाली को इलेक्ट्राॅनिक जनतंत्र द्वारा प्रतिस्थापित करने की कोशिश हो रही है। नतीजन, समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता दिनानुदिन बढ़ती ही जा रही है। अपने मूल दायित्वों से इतर मीडिया सिर्फ अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, जो औद्योगिक संस्कृति का मूल होता है। और एक सामान्य सी बात है कि किसी भी देश में कोई उद्योग तभी फल-फूल सकता है जब उसका वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था से बेहतर संबंध हो। इस बुनियादी परिप्रक्ष्य को ध्यान में रखकर देखें तो भारतीय मीडिया का पूरा चरित्र ही विरोधाभासी नजर आता है। एक ओर जहाँ उसे लोगों की विश्वसनीयता हासिल करने की चुनौती होती है वहीं दूसरी ओर पूँजीगत प्रवाह बनाए रखने के लिए सरकार की कृपा दृृष्टि की। बड़ी विचित्र स्थिति होती है- सरकार की अवहेलना की नहीं जा सकती और सरकार के एजेंट दिखने लगे तो साख पर संकट गहरा जाता है। इसलिए खबरों की प्रस्तुति इस तरह की जा रही है कि दोनों ही पक्षों को तुष्ट किया जा सके।
भले ही इस जद्धोजहद में मीडिया लोगों के सामने ऐसे सवालों को बहस के लिए रखता है, जो जनसरोकारों से कोसो दूर होते हैं । लेकिन उसकी प्रस्तुति ऐसी होती है कि लोग उसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उसपर अपनी राय भी देते हैं। आर्थिक मामलों में यह चलन अधिक बढ़ा है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में मीडिया शेयर बाजार में उठा-पटक, कंपनियों के मुनाफे, थोक मूल्य सूचकांक, वायदा बाजार जैसे पहलूओं को पैमाना मानकर विकास की अवधारणा तय करता है। उसे इस बात की फिक्र नही है कि आजादी के सात दशक बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोगो के पास सर छुपाने को घर नही हैं, बेरोजगारों की फौज बढ़ती ही जा रही है, लोग आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। भारतीय मीडिया के लिए ऐसे जमीनी मुद्दे विकास के पैमाने नहीं बन पाते हैं । ये तो सिर्फ ख़़बर है। और ऐसी ख़बरों की प्रस्तुति का अंदाज भी इतना नाटकीय होता है कि एकबार भी यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि हम समाचार देख-पढ़ रहे हैं या फिर मेलोड्रामा । और जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर जब कभी बहसें होती है तो उसे भटकाने की पूरी कोशिश की जाती है, सच्चाई जान बूझकर छुपाई जाती है।
एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की सोची-समझी रणनीति पूरे मामले को महत्वहीन बनाने के लिए पर्याप्त होता है। कारण स्पष्ट है- इन सबका संबंध राजनैतिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी उन मुठ्ठी भर लोगों से होता है जो अपने हितों को ही राष्ट्रीय हित समझते हैं। तभी तो अल्पसंख्यकों-दलितों की तुलना कुत्तों से करने वालों पर एकाध दिन भड़ास निकालने वाला मीडिया फिर से उन्हीं की शरण में होता है।
दरअसल इस पूरी स्थिति के लिए किसी एक पथ को जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी। भारतीय संदर्भो में इसकी पड़ताल दो कालखंडो में की जानी चाहिए। पहला कालखंड शुरू होता है जे0पी0 आंदोलन के समय से और दूसरा नब्बे के दशक से, जब भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण शुरू हुआ। जे0पी0 आंदोलन के बाद की स्थितियां भारतीय मीडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है या यूं कहें कि यहां से मीडिया का स्वरूप बिल्कुल बदल सा गया । इमरजेंसी के दौरान दमित पत्रकारिता, जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को पाने के लिए छटपटा रही थी। इस छटपटाहट ने जन संचार माध्यमों को राजनैतिक तौर पर सक्रिय बना दिया। पत्रकारों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ । गिरोहबंदी भी बढ़ी । अपनी महत्वाकांक्षा और राजनीतिक प्रतिबद्धता के वशीभूत सरकार के पक्ष विपक्ष में रिर्पोटिंग का चलन बढ़ा । इस तरह की रिर्पोटिंग ने मीडिया हाउसों को एक शक्ति केंद्र के रूप में उभारा । एक ऐसा शक्ति केंद्र जो जनमत को सरकार के पक्ष विपक्ष में खड़ा कर सकता था। हालांकि जनता पार्टी सरकार तक भी पत्रकारों में यह भ्रम की स्थिति बनी रही कि वे सत्ता पक्ष को अपना हीरो माने या विपक्ष को। लेकिन इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के मजबूत उभार ने इस धुंध को पूरी तरह खत्म कर दिया ।
पत्रकारों के लिए इमरजेंसी के दिन पीछे छुट चुके थें और राजनैतिक नेतृत्व का सामूहिक गुणगान होने लगा था। अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अंतिम दिनों में यह प्रवृति और अधिक देखी गई। यह बात अलग है कि एकपक्षीय कैम्पेन के बावजूद भी मीडिया महाधीश वाजपेयी जी को दोबारा सत्तासीन करवाने में पूरी तरह विफल रहे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। श्री सिंह ने दोबारा सत्ता संभाली। वर्ष 2013 लोकसभा चुनाव में मीडिया ने गोधरा कांड के कथित खलनायक नरेन्द्र मोदी को इस तरह प्रचारित किया जैसे उनके प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश का भाग्य पलट जाएगा। कैम्पेन रंग लाया। नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने।
दरसल यह एक बानगी भर है कि मीडिया किस तरह समयानुरूप अपने नायकों को चुनता है। और चयन का यह मानदंड तय होता है- मीडिया के काॅरपोरेट हितों के मुताबिक काॅरपोरेट हित- यही वह शब्द है जिसने नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के साथ ही मीडिया को सत्ता प्रतिष्ठानों के और अधिक नजदीक खड़ा किया। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ-साथ देश में सूचना-संचार क्रांति के एक नये युग का सुत्रपात भी हुआ। इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के क्षेत्र में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। इन कंपनियो ने भारत को एक उभरते बाज़ार के रूप में देख । एक ऐसा बाजार, जिसे अपनी जरूरतों के मुताबिक ढ़ाला जा सकता था। अन्य उद्योगों की तरह मीडिया भी नव पूंजीवाद की अंधी दौड़ में कुलांचे भरने लगा। इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी व्यवस्थाओं में स्वतंत्र और आदर्श पत्रकारिता की कोई गुंजाइश नहीं होती। परिणाम-छद््म स्वतंत्रता के माहौल में मूल्य चेतना से रहित पत्रकारिता के रूप में सामने है। अब ख़बरें दिखाई नहीं जाती बल्कि एजेंडा सेट किया जाता है। यह चलन इस कदर बढ़ा है कि अब मीडिया यह तय करने का काम कर रहा है कि समाज और राष्ट्र अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय करे। सबसे पहले यह तय होता है कि कौन सी सूचनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए । यदि किसी सूचना के संप्रेषण से बचना मुश्किल है तो उसे महत्वहीन बनाने की कोशिश की जाती है। विमर्श और बहस को किस दिशा में ले जाना है, यह तय किया जाता है। संक्षेप में कहें तो खबरों के साथ इस तरह से तालमेल किया जाता है कि लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं कि सूचना कहां खत्म हो रही है और राजनीति कहां से शुरू। यानि सत्ता समर्थक मीडिया लोगों को भ्रम की स्थिति में डालता है, जहां लोग पूरी तरह अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाते हैं।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नव पूंजीवाद के दौर में सत्ता समर्थक मीडिया के फैलते संजाल के बीच आधुनिक मानव समाज एक ट्रेजेडी सहने को अभिशप्त है। मीडिया और राजनीति के बीच के अंतर्संबधों की वस्तुनिष्ठ समझ के बिना जनसंचार माध्यमों की स्वतंत्रता और स्वायत्ता के वास्तविक निहितार्थ नहीं समझे जा सकते। इसके लिए सबसे जरूरी है- जनसंचार माध्यमों और उसके दर्शक-श्रोता-पाठक वर्ग के बीच विवेकपूर्ण आलोचनात्मक संबंधो का विकास हो। और जब तक ऐसे संबंधों का विकास नहीं हो जाता , यह कहना कहीं से भी उचित नहीं होगा की मीडिया का विस्तार लोकतंत्र का विस्तार है।
लेखक स्वतंत्र पत्रकार है।
मोबाइल-9430663831