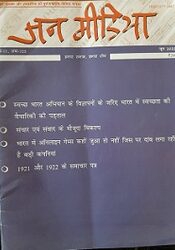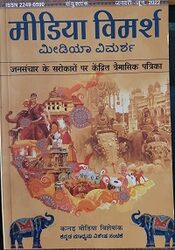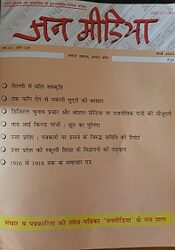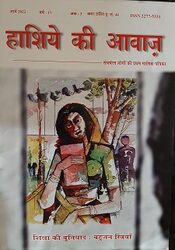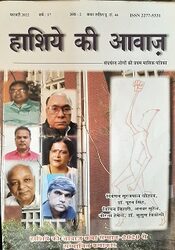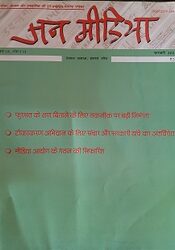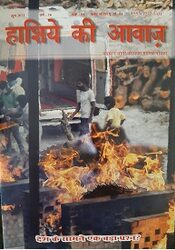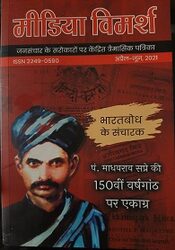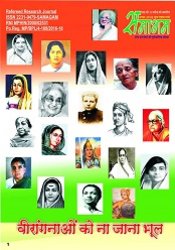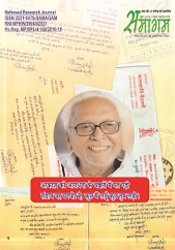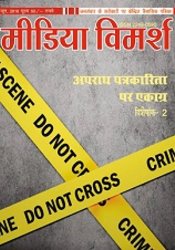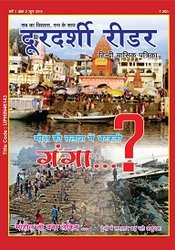संजय कुमार/ भारतीय मीडिया में मुकम्मल भारत की तस्वीर नहीं दिखती है। हिन्दी हो या अंगे्रजी या फिर उर्दू या कोई भाषा, देश-समाज की तस्वीर उसमें धुंधली दिखती है। ऐसे में भारतीय मीडिया की बात करें तो यह आरोपों के घेरे में है। हिन्दी, उर्दू और अंगे्रजी भारतीय मीडिया का चरित्र साफ नहीं है। इस मीडिया में मुकम्मल भारत की तस्वीर नहीं हैं, गांव नहीं है, हाशिये का समाज नहीं है। वजह साफ है इस मीडिया का अपना नजरिया। जो उसका मन होता है, जिससे फायदा दिखता है उसे ही परोसता है। मीडिया को अपने फायदे के आगे देश-समाज-गांव नहीं दिखता ?
संजय कुमार/ भारतीय मीडिया में मुकम्मल भारत की तस्वीर नहीं दिखती है। हिन्दी हो या अंगे्रजी या फिर उर्दू या कोई भाषा, देश-समाज की तस्वीर उसमें धुंधली दिखती है। ऐसे में भारतीय मीडिया की बात करें तो यह आरोपों के घेरे में है। हिन्दी, उर्दू और अंगे्रजी भारतीय मीडिया का चरित्र साफ नहीं है। इस मीडिया में मुकम्मल भारत की तस्वीर नहीं हैं, गांव नहीं है, हाशिये का समाज नहीं है। वजह साफ है इस मीडिया का अपना नजरिया। जो उसका मन होता है, जिससे फायदा दिखता है उसे ही परोसता है। मीडिया को अपने फायदे के आगे देश-समाज-गांव नहीं दिखता ?
मीडिया में आज हिन्दुस्तान की जो तस्वीर पेश की जा रही वह वर्ग विशेष पर फोकस रहता है। अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को नजरअंदाज किया जाता है। प्रिंट हो या इलैक्ट्रोनिक या फिर नया मीडिया सबसे ज्यादा राजनीतिक गलियारे की खबर को स्थान मिलता है। हद की बात यह है कि कुछ राजनेताओं का बयान फोटो के साथ रोजाना छापा/दिखाया जाता है। चुनाव के मौसम को छोड़ दें तो भी यह सिलसिला चलता रहता है। बिहार के मीडिया में कुछ नेता ऐसे है कि उनका वजूद नहीं होने के बावजूद उन्हें बयानों के आड़ में जगह मीडिया देती है। छपास के पीछे नेताओं का तर्क साफ रहता है कि उनके पार्टी का स्टौंड तो रखना है। वहीं, मीडिया संतुलन की बात कर पल्ला झाड लेती है। बड़े नेताओं की बात तो समझ में आती है लेकिन छुटभैया नेता का क्या? मीडिया मैनज के इन योद्धाओं की चलती है। इनके इशारे पर पे्रस वार्ता संचालित होता है और कैमरे का फोकस भी इन पर साफ रहता है।
उदाहरण के लिए मीडिया के कैनवास को खंगालने की जरूरत नहीं खुद ब खुद दिख जाता है। वहीं मुद्दे की बात हो। समाज के अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति की बात हो तो इनके बयान ढूंढ़ते रह जायेगंे। हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले में दलितों पर दबंगो के कहर पर चुप्पी दिखी तो वहीं अक्दूबर2015 में ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक दलित परिवार के महिला व पुरूषों को न्याय की गुहार महंगी लगी। पुलिस ने सब को भरे समाज के सामने नंगा किये जाने की घटना पर मीडिया के मुखर तेवर की जगह, हर ओर खामोशी थी, वहीं गोमांस, आरक्षण और जाति के मुद्दे पर एक दूसरे पर बयानों से हमला बोलते रहे। जाहिर है राजनीतिक फायदा महत्वपूर्ण है। वहीं, मीडिया भी जो बिकता है उसे बेचने से परहेज नहीं करती भले ही उससे समाज-देश को नुकसाान क्यों न हो! जाहिर सी बात है देश-समाज के विकास की बात करने वाली मीडिया आज व्यक्ति विशेष, सरकार और राजनीति को दायरे में लिए हुए है। एक वक्त था जब सरकार की जन नीतियों को जगह दी जाती थी। आज वह विज्ञापन तक ही सिमट चुका है। सरकार और मीडिया के बीच सांमजस रखने वाला पीआईबी के पीछे एक समय सरकारी खबरों के लिए घूमने वाले पत्रकारों को अब नहीं के बराबर देखा जाता है।
राजनीति के बाद अपराध पर मीडिया का फोकस दिखता है। अपराधी का महिमामंडल आम बात है उस पर अगर वह बाहुबली नेता हो तो क्या कहने। मीडिया के लिए वह कोई महंगा आइटम हो जाता है। मीडिया में जिस तरह से खेल, सिनेमा, आर्थिक का पेज/जगह दिया जाता है, उसी तरह सामाजिक मुद्दों के लिए जगह मिलने से भारत की तस्वीर दिखती। हालांकि गाहे बगाहे कुछ खबरें हस्तक्षेप करती दिखती है लेकिन जो सरोकार होना चाहिये वह नहीं दिखता। समाज की तस्वीर यानी हिन्दुस्तान की तस्वीर। 85 प्रतिशत वह समाज जो आज भी हाशिये पर है। हाशिये के समाज को मीडिया द्वारा नजरअंदाज करने की बात हाल फिलहाल की नहीं है। वर्षो से यह सब हो रहा है। कहने के लिए समाज बदल गया है, बदल रहा है। हकीकत कुछ और है। वहीं परोसा जाता है जो न्यूज रूम चाहता है। और इसकी संरचना को बनाने वाला समाज का वंचित वर्ग नहीं बल्कि सवर्ण वर्ग है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इसके पीछे राष्ट्रीय न्यूज रूम की संरचना का जातिवादी होना मानते हैं। राष्ट्रीय सर्वे का हवाला देते हुए बताते हैं कि भारतीय मीडिया अपनी संरचना में हिन्दू है, सवर्ण है और पुरूष है। फैसला लेने वाले किसी पद पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को कोई नहीं था। पिछड़े मात्र चार प्रतिशत थे। जबकि सामाजिक संरचना में देश की आबादी में हिस्सेदारी 85 फीसदी से ज्यादा इनकी है। सिर्फ एक जाति ब्राहमण का इन पदों पर 49 फीसदी कब्जा पाया गया। भारतीय न्यूज मीडिया की सामाजिक हकीकत बेहद कड़वी है। यह सवर्ण दिंदुओं की सवर्ण हिंदुओं के हित में संचालित संस्था है(देंखे-‘‘हिंदु सवर्ण पुरूष मीडिया’’ दिलीप मंड़ल, शुक्रवार 1 से 15 सितंबर 2015)।
न्यूज रूम की संरचना और उसके निर्णय से साफ है कि भारतीय न्यूज मीडिया की सामाजिक हकीकत बेहद कड़वी है। योगेन्द्र यादव और अनिल चमड़िया की टीम ने सर्वे कर इसका खुलासा वर्षो पूर्व किया था। कई साल बीतने के बाद भी हालात नहीं बदले है। मीडिया में क्या जायेगा क्या नहीं पहले संपादक तय कर लेते थे लेकिन आज पूरी पकड़ प्रबंधक या प्रबंधक संपादक की है। सरकारी मीडिया में तो सब तय है वहीं निजी मीडिया में भी यह सब तय है। हालांकि मीडिया का जबरदस्त विस्तार हुआ है।
उर्दू के चर्चित लेखक और पटना से छपने वाला उर्दू दैनिक पिंदार के संपादक रेहान गनी कहते हैं, ‘उर्दू अखबारों में भी भारत की मुकम्म्ल तस्वीर गायब है। अगर मुसलमनों की बात करें तो यहां अंतिम कतार में खड़े जो है वे उपेक्षित है। उर्दू मीडिया इनकी आवाज बनने की जहमत नहीं उठाता है। मुसलमानों को मुख्यधारा में लाने के लिए सक्रिय संस्थान जब नहीं झाकते तो उर्दू अखबार की तो बात ही भूल जाये।
भले ही भारतीय मीडिया में भारत की मुकम्म्ल तस्वीर न दिखे लेकिन आज मीडिया ने अपनी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट से कलर बना ली है। वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक हिन्दुस्तान के संपादक शशि शेखर की माने तो, 1980 के दशक में पत्रकारिता मूलतः महानगरीय और कस्बाई हिस्सों में बांटी जा सकती थी, पर आज मीडिया समूहों ने बहुत विस्तार कर लिया है। कुछ समीक्षक इनकी तुलना साम्राज्यों से करते हैं। इस चलन ने अगर कुछ सवाल खड़े किए हैं, तो पत्रकारिता का भला भी किया है। बहुत से नौजवानों को अब इज्जत के साथ आजीविका कमाने का अवसर मिलता है। इसीलिए बड़ी संख्या में नौजवान पत्रकारिता को पेशे के तौर पर अपनाना चाहते हैं। मीडिया समूहों का विस्तार भी सवालों के घेरे में है। पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार के लिए आमंत्रण मूल्य और उपहार दिए जाते हैं। टीवी चैनल ऑपरेटर्स को डिस्ट्रीब्यूशन फी के अलावा भी फायदा देते हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। इससे लाभ-हानि का नया समीकरण पैदा हुआ है, जो तेवरदार पत्रकारिता के लिए खतरा बन सकता है (देखें-‘35 साल बाद हिन्दी मीडिया’, दैनिक हिन्दुस्तान,19 सितंबर2015)।
जाहिर है मीडिया हाउस पैसे बनाने की दिशा में सक्रिय है। पत्र और पत्रकारिता दलाली के आरोपों के घेरे में है। ऐसे में सामाजिक सरोकार का पीछे छूटना? मीडिया में भारत की वास्तविक तस्वीर का गायब होना स्वाभाविक है? तभी तो ‘द हिंदू’ के पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन अक्सर कहते रहते हैं कि जर्नलिस्ट को एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। उनका मानना है कि एक्टिविस्ट अपनी एक धारण को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं, जबकि पत्रकार को हमेशा संतुलित रह कर रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। पत्रकार के अंदर काम के प्रति पैशन होना अत्यंत आवश्यक है। श्री वरदराजन मानते है कि भारत में मीडिया का बहुत विशाल स्वरूप है। बड़ी संख्या में अखबार, के साथ-साथ चैबीस घंटे चलने वाले सैकड़ों चैनल हैं, पर सचाई यह है कि इनमंे से नब्बी फीसदी नुकसान में ही है। जिन समूहांे के बाद एंटरटेनमेंट चैनल है, वे ही रेवेन्यू बना पाते हैं। वे कहते हैं अब मीडिया, विज्ञापन का व्यवसाय बन गया है। एक बड़े अंग्रेजी अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर का तो खुले तौर पर कहना है कि हम ऐडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में काम करते हैं। श्री सिद्धार्थ कहते हैं, आज विज्ञापनों के आधिपत्य के चलते रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लिखी गई खबरों को भी सही स्पेस नहीं मिल पाता है। आजकल सब कुछ इतना इकॉमिक ड्रिवन और पॉलिटिकली ड्रिवन हो गया है कि बड़े मीडिया हाउस छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान हुई महिलाओं की मौत पर खबर करने के लिए पत्रकार नहीं भेजते हैं, पर मैडिसन स्क्वायर पर पीएम की स्पीच कवर करने के लिए सभी के संवादादाता वहां मौजूद रहते हैं (देखें-‘जर्नलिस्ट को एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए’ समाचार4मीडियाडाॅटकाॅम,8 अक्टूबर2015)।
वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन की बातें हकीकत है। भारतीय मीडिया का जहंा जन सरोकार पीछे छूटता जा रहा हैं,वहीं सेलिबे्र्रटी-बिकाउ खबरों के पीछे मीडिया हाउस बीन बचाता घूम रहा है। जमीनी स्तर पर यह स्थिति बनी हुई है कि दलित और आदिवासी हाशिये के समाज के लोग हैं। हाशिये के समाज के लोग इन माध्यमों में आते हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। पुस्तक ‘अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया’ जो भारत के ग्यारह राज्यों के सर्वे पर आधारित है। सर्वे में कहा गया है कि भारतीय समाज में किस-किस तरह से दलितों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। सर्वे बताता है कि आज भी भारत के 80 प्रतिशत गांव में किसी न किसी रूप में दलितों के साथ अछूत सा व्यवहार किया जाता है। पंचायत में नीचे बैठने को कहा जाता है। मीड डे मील को लेकर भेदभाव किया जाता है। चार में से एक गांव आज भी ऐसे है जिनमें नये कपड़े, छाता लेकर चलने और चश्मा लगाने, जूता पहनकर चलने पर दलितों को रोक है। शहर के दलितों के साथ शायद ऐसा नहीं हो! लेकिन आज भी यह हो रहा है। भारतीय समाज में खासकर दक्षिण भारत में कई ऐसे जगह है जहां पर ढाबों में दलितों के लिए अलग से बर्तन रखे जाते हैं। यह कहा जाता है कि आज ग्लोबलाइजेशन हुआ है मार्केट तंत्र आया है इससे कुछ सामाजिक समानता आई है। लेकिन जमीनी सच यह है कि आज भी गाँव के बाजार में जब दलित जाता है तो उसके साथ उसकी जातिगत पहचान बनी रहते है। दूसरे लोगों की तरह वह सामानों को अपने हाथ में उठा-उठा कर, देखकर खरीद नहीं सकता, उसे दूर से ही दुकानदार को बताना होता है। सर्वे आधारित ये जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे आज के ग्रामीण भारत के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। यह सच हमारे अखबारों में नहीं छपता। हिन्दी अखबारों में तो बिल्कुल नहीं। हिन्दी अखबारों में दलित तब उपस्थित होता है जब कोई बस्ती या गांव जला दिया जाता है। आज सांप्रदायिकता को तो बड़े खतरे के रूप में पहचाना गया लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है दलितों के साथ भेदभाव । यह भारतीय समाज का सच है। अंधेरे भारत का सच है, जो हमारे भारतीय मीडिया में अनुपस्थित है ।
80 के दशक को देखें तो उस वक्त का मीडिया सामाजिक सारोकारों का भारतीय मीडिया था। उसमें समाज रहता था। 90 के दशक तक वह बहुत व्यवसायी हो गया। दो हजार दशक में आते-आते पूरा व्यवसायिक हो जाता है और आज 2015 में तो वह बाजार हो गया है। और बाजारवादी भारतीय मीडिया से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जहंा खबरंे गढ़ी जाती हैं और जो खबर है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
देखा जाये तो भारत के परिपेक्ष में राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली पर सामाजिक जनतंत्र ? यह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। वह है सामाजिक जनतांत्रिकीकरण मीडिया में वंचितों का मुद्दा। सवाल उठता है कि जो मुख्यधारा का मीडिया है उसे जनतांत्रिक कैसे बनाया जाये। इस मुख्यधारा के मीडिया में वंचित या अंतिम कतार के व्यक्ति की सम्मानजनक व प्रभावकारी उपस्थति दर्ज कैसे की जाये? यह भी एक बड़ा सवाल है। ताकि भारत की मुकम्म्ल तस्वीर साफ-साफ मीडिया में दिखे।
\(लेखक इलैक्ट्रोनिक मीडिया से जुड़े हैं- मो 9934293148)।