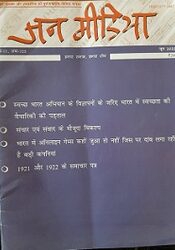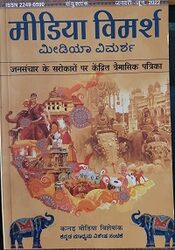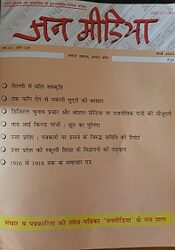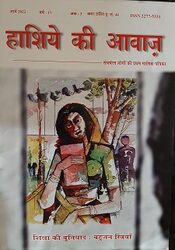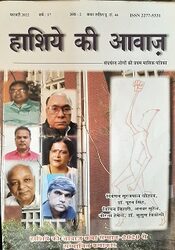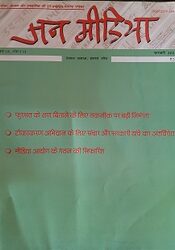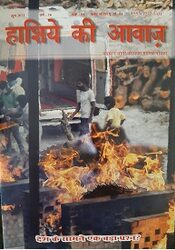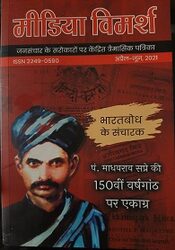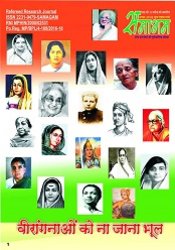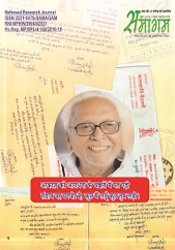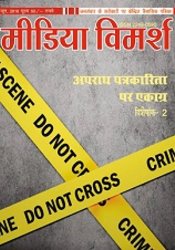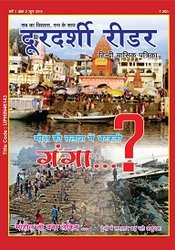बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों का अचानक नौकरी से बाहर किया जाना हमारे मीडिया के लिए खबर का विषय नहीं लगा
उर्मिलेश / स्वतंत्रता दिवस के ठीक एक दिन बाद का शुक्रवार देश के एक बड़े टीवी घराने टीवी-18 के सैकड़ों पत्रकारों, गैर-पत्रकार कर्मियों के लिए काला दिन साबित हुआ. लेकिन शुक्रवार के चैनल-समाचारों या शनिवार के अखबारों में टीवी-18 में बड़े पैमाने पर हुई खास तरीके की छंटनी(कुछ महीने का वेतन-भुगतान कर इनसे इस्तीफा ले लिया गया) के बारे में कोई खबर नहीं थी. इतनी बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों का अचानक नौकरी से बाहर किया जाना हमारे मीडिया के लिए खबर का विषय नहीं लगा. सबकी खबर लेने वाले, अपनी खबर नहीं लेते और न देश-समाज को देते हैं. यह हमारे मीडिया का रिवाज सा बन गया है.
सिर्फ अंग्रेजी अखबार ‘द हिन्दू’ और ‘मिंट’ ने पिछले दिनों यह खबर विस्तार से छापी थी कि टीवी-18 के सीएनएन-आईबीएन, सीएनबीसी-टीवी 18 और आईबीएन-7 के अंदर खर्च में कटौती के लिए पुनर्संरचना और आकार में कटौती पर काम चल रहा है. ‘हिन्दू’(16 अगस्त) की खबर में बताया गया कि चैनल के प्रबंधन ने अपने खर्च में 30 फीसदी कटौती करने के लक्ष्य से प्रेरित होकर यह कदम उठाया. इसके तहत लगभग 350 कर्मियों की सेवाएं जा सकती हैं. उल्लेखनीय है कि इस चैनल-समूह को अब देश का एक बड़ा कारपोरेट घराना अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित और संचालित करता है. पिछले वर्ष चैनल के स्वामित्व और शेयर-हिस्सेदारी में बड़े फेरबदल के बाद से ही इसके प्रबंधकीय कामकाज की शैली में खास ढंग का बदलाव दिखने लगा था. कहा जा रहा है कि कुछ प्रबंधकीय-अंतर्विरोधों के चलते ही चैनल के सीईओ डी वेंकटरमन ने पिछले दिनों इस्तीफा दे दिया.
सच पूछिए तो देश के मीडिया उद्योग के लिए मानों कोई नियम-कानून नहीं हैं. बड़े संपादक-पत्रकार भी नियंत्रण या रेगुलेशन के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं, पर वे कतई यह सवाल नहीं उठाते कि मीडिया की स्वतंत्रता या स्वनियंत्रण की बात सिर्फ लिखने-बोलने के मामले के लिए है, मीडिया-बिजनेस के लिए नहीं. मीडिया-मालिक और उनकी कठपुतलियों के तौर पर काम करने वाले प्रबंधकनुमा संपादक शायद भूल गए हैं कि हमारे देश में एक ‘श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मी कानून-1955’ भी है. इसे सरकार या संसद ने अभी खत्म नहीं किया, इसका अस्तित्व बरकरार है, पर सच यह है कि इस कानून का कोई नामलेवा नहीं बचा है.
इससे पहले भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, पटना, रांची, लखनऊ, भोपाल, रायपुर, बंगलुरू सहित देश के विभिन्न नगरों-महानगरों के विभिन्न मीडिया संस्थानों में पत्रकारों और गैर-पत्रकार मीडियाकर्मियों की छंटनी हुई है, उनसे जबरन इस्तीफे लिए गए हैं, संस्थानों में बंदी हुई है या ब्यूरो बंद किए गए हैं. बंगाल के एक विवादास्पद मीडिया संस्थान-शारदा समूह का मामला कुछ ही महीने पहले उजागर हुआ. शारदा समूह के चैनलों की बंदी के मामले में चिटफंड का धंधा करने वाली एक कंपनी और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेताओं की मिलीभगत भी सामने आई. इस समूह के हजार से अधिक पत्रकार और गैर पत्रकार कर्मचारी सड़क पर बताए जाते हैं. एक मोटे अनुमान के मुताबिक बीते दस सालों में भारतीय मीडिया उद्योग में दस हजार से अधिक पत्रकारों-गैरपत्रकार मीडियाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. मीडिया के मामले में देश के श्रम कार्यालयों और कानूनों के पूरी तरह मृतप्राय होने के चलते पत्रकार-गैरपत्रकार कर्मियों की बेरोजगारी या उनके सेवा से हटाए जाने के बारे में कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं आ सका है. मीडिया समूहों में ठेकेदारी व्यवस्था के बढ़ते दबदबे के चलते अब यूनियनें भी खत्म हो गई हैं, इसलिए उनसे भी सही आकड़े नहीं मिल सकते. अखिल भारतीय पत्रकार यूनियन अब खंड-खंड होकर यूनियन के नाम पर सिर्फ कंकाल रह गई हैं. कुछेक इलाकों में अगर कोई यूनियन सक्रिय है, तो सिर्फ वहां के आंकड़े ही उनसे मिल सकते हैं. सरकार और पक्ष-विपक्ष के राजनेताओं को मीडिया उद्योग के मौजूदा परिदृश्य के बारे में सबकुछ मालूम है, पर सच यह है कि वे पत्रकारों या कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते. यह महज संयोग नहीं कि टीवी-18 की अफसोसनाक खबर पर मनमोहन से मोदी तक, किसी ने अब तक अफसोस तक नहीं जताया. दरअसल, हमारे राजनेता-हुक्मरान मीडिया के नाम पर सिर्फ मालिकों के बारे में ही सोचते हैं. यही कारण है कि बीते दस सालों में शायद ही सरकारों या उनके श्रम विभागों ने बड़े मीडिया संस्थानों में छंटनी या जबरन इस्तीफा लेने के मामले में कभी कोई हस्तक्षेप किया हो. सरकारों की रूचि मीडिया संस्थानों के मालिकों को फायदा पहुंचाकर स्वयं फायदा वसूलने में है. इससे पहले, देश के ज्यादातर बड़े मीडिया समूहों में भी अनेक पत्रकारों-गैरपत्रकार कर्मियों की नौकरियां जा चुकी हैं. पर सरकार के स्तर पर कोई बड़ी पहल नहीं दिखी. जब 2004-5 के दौरान देश के एक बड़े अखबारी घराने के दिल्ली स्थित मुख्यालय में एक साथ 360 से अधिक गैर-पत्रकार मीडियाकर्मी निकाले गए थे, तो वहां काम कर रहे पत्रकारों ने दफ्तर के सामने धरना-प्रदर्शन कर रहे कर्मियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया. उन्हें लगा कि पत्रकार तो कुछ बड़ी चीज होता है, उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी. पर जल्दी ही समूह के हिन्दी और अंग्रेजी अखबार के पत्रकारों पर भी गाज गिरने लगी. संस्थान की कथित ताकतवर यूनियन यकायक ताश के पत्तों की तरह ढह गई. उसके ज्यादातर नेता पट चुके थे. नब्बे फीसदी पत्रकारों को उनकी नियमित सेवा(श्रमजीवी पत्रकार कानून और वेतन बोर्ड के तहत) से हटकर ठेके पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया. पहले ग्रुप के हिन्दी अखबार में और फिर अंग्रेजी अखबार में इसे किसी योजनाबद्ध ऑपरेशन की तरह अंजाम दिया गया. पहले चरण में जिन कुछ लोगों ने ठेके पर जाने से इंकार किया, उन्हें काम से वंचित किया जाने लगा. बाद में उन्हें निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ कहा गया कि वे अब भी ठेके पर आ जाएं तो नौकरी बच सकती है. वही हुआ, सभी लोग ठेके पर आ गए. उनके वेतन में कोई खास बढ़ोत्तरी भी नहीं हुई. बाद में कइयों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. उस दौर में समूह के विभिन्न प्रकाशनों के सैकड़ों पत्रकारों-गैरपत्रकार कर्मियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा. उसके बाद तो दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में स्थित मीडिया घरानों में पत्रकार-गैरपत्रकार कर्मियों की छंटनी या उन्हें नियमित सेवा से ठेके पर लेने और फिर उसमें एक बड़े हिस्से को बाहर निकालने का सिलसिला सा शुरू हो गया. एक अनुमान के मुताबिक सन 2008-09 में देश के विभिन्न मीडिया घरानों के कम से कम 6000 पत्रकार-गैरपत्रकार कर्मी बेरोजगार हुए. अभी कुछ ही महीने पहले देश के 13 राज्यों में कई-कई संस्करण निकालने और 75 लाख पाठकों का दावा करने वाले दैनिक भास्कर समूह से कई पत्रकारों को बाहर किया गया या उन्हें इस्तीफा देकर मामूली भुगतान के बाद बाहर चले जाने को कहा गया. जिन दो पत्रकारों ने इस्तीफा देने से इंकार किया, उन्हें बाहर जाने का नोटिस थमा दिया गया. इनमें एक सहयोगी संपादक स्तर के पत्रकार जितेंद्र कुमार ने भास्कर समूह के नौकरी से निकालने के फैसले को चुनौती दी है. जितेंद्र के मुताबिक मामला श्रम कार्यालय में लंबित है. बड़ी तेजी से उभरे इस मीडिया समूह या इससे सम्बद्ध कंपनियों का धंधा खनन, ऊर्जा, रियल स्टेट, कोयला सहित कई क्षेत्रों में पसरा हुआ है.
सच पूछिए तो देश के मीडिया उद्योग के लिए मानों कोई नियम-कानून नहीं हैं. बड़े संपादक-पत्रकार भी नियंत्रण या रेगुलेशन के नाम पर नाक-भौं सिकोड़ते हैं, पर वे कतई यह सवाल नहीं उठाते कि मीडिया की स्वतंत्रता या स्वनियंत्रण की बात सिर्फ लिखने-बोलने के मामले के लिए है, मीडिया-बिजनेस के लिए नहीं. मीडिया-मालिक और उनकी कठपुतलियों के तौर पर काम करने वाले प्रबंधकनुमा संपादक शायद भूल गए हैं कि हमारे देश में एक ‘श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मी कानून-1955’ भी है. इसे सरकार या संसद ने अभी खत्म नहीं किया, इसका अस्तित्व बरकरार है, पर सच यह है कि इस कानून का कोई नामलेवा नहीं बचा है. इसका उपयोग या क्रियावन्यन देश में शायद ही कहीं ठीक से हो पा रहा है. वजह, मीडिया में हर जगह(कुछेक अपवादों को छोडकर) ठेकेदारी प्रथा लागू हो चुकी है. ऐसे में मीडिया समूहों के मालिक किसी कानून से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं, उन्होंने अपने लिए ठेके के दस्तावेजों के अनुसार अपनी सहूलियत के कानून बना लिए हैं.
देश की संसद ने पहली बार 20012-13 में मीडिया से जुड़े इस तरह के मुद्दों को गंभीरतापूर्वक लिया और सारे पहलुओं पर गौर करने के बाद सम्बद्ध मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की एक रिपोर्ट सामने आई. संसद में पेश की गई सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बद्ध इस समिति की 47वीं रिपोर्ट पर अब सरकार को पहल लेनी है. कई महीने बीतने के बाद भी सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई है. संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि सभी मीडिया समूहों में पत्रकारों आदि के लिए श्रमजीवी पत्रकार कानून-1955 का कड़ाई से पालन किया जाय. यानी, संसदीय समिति ने मीडिया समूहों में पत्रकारों को ठेके पर नियुक्त किए जाने के रिवाज को खारिज किया है. क्रॉस-मीडिया होल्डिंग से लेकर पेड न्यूज और विज्ञापन के नाम पर कंटेट से खेल, प्राइवेट ट्रिटीज और पाठकों-दर्शकों के साथ धोखाधड़ी जैसे अनेक मुद्दों पर समिति की सिफारिशें प्रासंगिक और उपयोगी हैं. क्या सरकार मीडिया क्षेत्र में हाहाकार मचने से पहले संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल करेगी या 2014 के संसदीय चुनावों के मद्देनजर केंद्र-राज्यों की सरकारें और बड़े राजनीतिक दल मीडिया-मालिकों को नाराज नहीं करना चाहते?
(गुलेल डॉट कॉम से साभार )